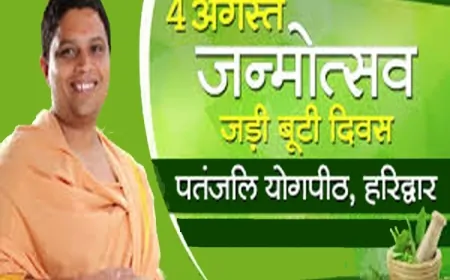उत्तर प्रदेश में पुलिस अत्याचार और जवाबदेही का संकट : संस्थागत लापरवाही व सुधार की आवश्यकता
उत्तर प्रदेश में पुलिस अत्याचार और जवाबदेही का संकट गहराता जा रहा है। FIR दर्ज न करना, हिरासत में मौतें, मुठभेड़ हत्याएं और संस्थागत लापरवाही से न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यह लेख केस स्टडीज़, सामाजिक प्रतिक्रियाओं और न्यायिक हस्तक्षेपों के आधार पर पुलिस सुधार के व्यावहारिक समाधान सुझाता है।
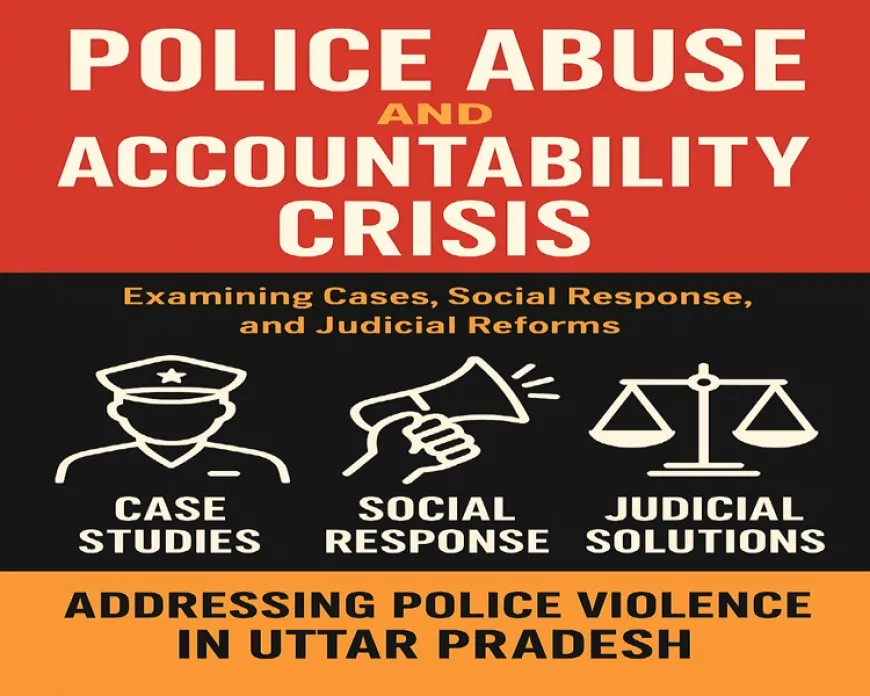
उत्तर प्रदेश (और व्यापक रूप से भारत) में पुलिस अत्याचार, संस्थागत लापरवाही तथा जवाबदेही की कमी जैसे संज्ञेय अपराधों की FIR दर्ज न करना, शिकायतकर्ताओं/पत्रकारों का उत्पीड़न, 'मुठभेड़ों' में हत्याएँ, हिरासत में मौतें एक दीर्घकालिक संकट का रूप ले चुकी हैं। अदालतों ने बार-बार मानक तय किए, पर ज़मीन पर पालन टुकड़ों-टुकड़ों में दिखाई देता है। इस संपादकीय में हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, हालिया क़ानूनी बदलावों, निगरानी संस्थाओं की भूमिका, कुछ ताज़ा उदाहरणों/आँकड़ों और उत्तर-प्रदेश उन्मुख सुधार-रोडमैप पर केंद्रित, तथ्याधारित विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।
क़ानूनी कसौटियाँ: अदालतों ने क्या कहा है
संज्ञेय अपराध में FIR अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट ने Lalita Kumari v. Govt. of UP (2013) में स्पष्ट किया कि संज्ञेय अपराध का प्राथमिक दृष्टया संकेत मिले तो FIR दर्ज करना पुलिस का दायित्व है, कुछ श्रेणियों में सीमित प्रारम्भिक जाँच की गुंजाइश है, पर FIR टालने का अधिकार नहीं।
गिरफ़्तारी/हिरासत में सुरक्षा: D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) में गिरफ़्तारी-हिरासत के 11+ मानक अरेस्ट मेमो, परिजनों को सूचना, मेडिकल जाँच, आदि बाध्यकारी बनाए गए।
मुठभेड़ों पर 16 दिशानिर्देश: PUCL v. State of Maharashtra (2014) ने ‘एन्काउंटर डेथ’ में तत्काल FIR, स्वतंत्र जाँच (आमतौर पर CID/अन्य इकाई द्वारा), मजिस्ट्रियल इनक्वायरी, हथियारों की फॉरेंसिक जाँच, और जांच पूरी होने तक पदक/तुरंत पदोन्नति पर रोक जैसे निर्देश दिए, ये कानून के समान बाध्यकारी हैं। बाद के आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा-निर्देशों की बाध्यता दोहराई।
थानों में CCTV व ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग: Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh (2020) में देश-भर के थानों/जांच कक्षों में CCTV (ऑडियो सहित) लगाने और निगरानी-समिति बनाने का आदेश दिया गया।
पुलिस सुधार का संवैधानिक फ्रेम: Prakash Singh v. Union of India (2006) में राज्य सुरक्षा आयोग, DGP की निश्चित कार्यावधि, जांच व क़ानून-व्यवस्था का संगठनात्मक पृथक्करण, एवं Police Complaints Authority (PCA) जैसी संस्थाएँ अनिवार्य की गईं, पर अनुपालन व्यापक रूप से अधूरा है।
नए आपराधिक प्रक्रिया ढाँचे में अवसर
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसके धारा 173 के तहत ई-FIR/इलेक्ट्रॉनिक सूचना, ज़ीरो-FIR (अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी थाने में), तथा कुछ मामलों में प्रारम्भिक जाँच को विधिक रूप मिला, शर्त यह कि हस्ताक्षर/पुष्टि समयबद्ध हो और रिकॉर्ड तुरन्त न्यायालय/उच्चाधिकारियों तक पहुँचे। यह पीड़ित-केंद्रित, समयबद्ध और डिजिटल ट्रेल-आधारित जवाबदेही का अवसर देता है।
तथ्य-आधार: हिरासत में मौतें व रिपोर्टिंग दायित्व
NHRC को 24 घंटे में सूचना: 1993 से NHRC ने निर्देशित किया है कि किसी भी हिरासती मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर दी जाए; पोस्ट-मार्टम की वीडियोग्राफी व मजिस्ट्रियल जाँच रिपोर्ट भी भेजनी होती है। कई राज्य/ज़िले आज भी इसमें ढिलाई करते पकड़े गए हैं।
संख्या और प्रवृत्तियाँ: हालिया आकलनों में 2024 में भारत में कुल \~2,700+ हिरासती मौतें (न्यायिक+पुलिस) दर्ज होने का उल्लेख है; 2016-22 के बीच 11,650+ हिरासती मौतों का समेकित अनुमान भी उद्धृत है। यह आँकड़े संस्थागत जवाबदेही की कमी पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं।
उल्लंघन पर नोटिस: NHRC ने अनेक मामलों में 24 घंटे की रिपोर्टिंग न होने पर राज्य सरकारों/पुलिस प्रमुखों को नोटिस दिए, यह बताता है कि प्रक्रियात्मक अनुपालन ही बड़ी समस्या है, केवल कानून की कमी नहीं।
नोट: NCRB की Crime in India 2022 रिपोर्ट भी हिरासती अपराध/मौतों के पैटर्न पर संकेत देती है, पर रिपोर्टिंग-गैप्स के कारण असल संख्या अधिक हो सकती है।
केस-स्टडी स्नैपशॉट्स
1. मुठभेड़ों में मौतें: PUCL (2014) दिशा-निर्देशों के बावजूद, जाँच की स्वतंत्रता/समयबद्धता और पारदर्शिता असमान है; सुप्रीम कोर्ट ने हाल में भी दोहराया कि ये प्रोटोकॉल बाध्यकारी हैं, पर अनेक मामलों में FIR/स्वतंत्र SIT/मजिस्ट्रियल जांच की गुणवत्ता पर सवाल बने रहते हैं।
2. कमज़ोर वर्गों/महिलाओं की शिकायतें: Lalita Kumari का सिद्धान्त (FIR अनिवार्य) और BNSS की ई-FIR/ज़ीरो-FIR व्यवस्था मैदान-स्तर पर अक्सर 'प्रारम्भिक जाँच' के नाम पर टाल दी जाती है; नतीजन शिकायतें लंबित/ठुकराई जाती हैं। कुछ राज्यों/ज़िलों ने हाल में शिकायत-संवाद दिवस जैसी पहलें शुरू की हैं, जिनका व्यवस्थित विस्तार उपयोगी हो सकता है।
3. NHRC/NCW की कार्यवाही: NHRC का 24-घंटे रिपोर्टिंग-मानक व मजिस्ट्रियल जाँच SOP तो मज़बूत हैं, पर कई बार आयोग राज्यों की एकतरफ़ा रिपोर्ट पर निर्भर दिखता है; NCW ने 2023 SOP के ज़रिए शिकायत-प्रक्रिया मानकीकृत की मैदानी सुनवाई/काउंसलिंग/पुलिस-अनुवीक्षण शामिल पर राज्य महिला आयोगों की निष्क्रियता/रिक्ति के समय, राष्ट्रीय आयोग पर असमान्य भार पड़ जाता है।
4. CCTV/ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग: Paramvir Singh (2020) के बाद भी 100% कवरेज, रख-रखाव, और फुटेज-सुरक्षा (चेन-ऑफ-कस्टडी) में महत्वपूर्ण गैप हैं, जो हिरासती अत्याचार के मामलों में साक्ष्य-संकलन को कमजोर करते हैं।
5. पुलिस सुधारों का अनुपालन: Prakash Singh (2006) के 18+ साल बाद भी अधिकांश राज्यों में DGP नियुक्ति प्रक्रिया/स्थिरता, राज्य सुरक्षा आयोग, और विशेष रूप से Police Complaints Authority का ढाँचा काग़ज़ पर है या दंत-रहित है, स्वतंत्र सचिवालय/समन शक्ति/अनुशासनात्मक परिणाम अक्सर अनुपस्थित हैं।
समाधान: न्यायिक-संवैधानिक, प्रशासनिक, सामाजिक एक समेकित रोडमैप
(A) विधिक/न्यायिक
1. PUCL-अनुपालन की जीरो-टॉलरेंस नीति: हर 'एन्काउंटर डेथ' में स्वतः FIR u/s 302 समतुल्य, स्वतंत्र SIT/CID से जाँच, 3–4 महीने में मजिस्ट्रियल जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक पोर्टल पर। अनुपालन-विलंब पर कंटेम्प्ट/विभागीय दंड का स्पष्ट प्रावधान।
2. FIR-अधिकार का प्रवर्तन: Lalita Kumari + BNSS-धारा 173 के अनुरूप ई-FIR/ज़ीरो-FIR को बाध्यकारी SOP के साथ; इलेक्ट्रॉनिक सूचना की प्राप्ति-रसीद, 24 घंटे में FIR-कॉप़ी, और अस्वीकार होने पर कारण-बताओ नोटिस व रिव्यू-मैकेनिज़्म।
3. हिरासत-सुरक्षा: D.K. Basu और Paramvir Singh अनुपालन का थर्ड-पार्टी ऑडिट CCTV की 30–90 दिन सुरक्षित स्टोरेज, ऑडियो-वीडियो इंटेरोगेशन रूम, मेडिकल-स्क्रीनिंग की ई-लॉगबुक।
(B) संवैधानिक/संस्थागत
4. Police Complaints Authority (PCA) को दंत-नख: Prakash Singh के अनुरूप स्वतंत्र चेयर, चयन-समिति, समन/जाँच/सिफ़ारिश-बाध्यकारी बनें; PCA-डैशबोर्ड पर शिकायत, कार्यवाही-स्थिति, और अनुपालन-रेटिंग सार्वजनिक हों।
5. NHRC/NCW की जाँच-स्वायत्तता: एकतरफ़ा पुलिस रिपोर्ट पर निर्भरता घटे फोरेंसिक/चिकित्सकीय विशेषज्ञ पैनल, ऑन-स्पॉट फैक्ट-फाइंडिंग टीम, और 24-घंटे रिपोर्टिंग उल्लंघन पर राज्य-वार पेनल्टी इंडेक्स सार्वजनिक किया जाए।
(C) प्रशासनिक/संचालन
6. डिजिटल ट्रेसिबिलिटी: BNSS के तहत e-FIR/Zero-FIR का राज्य-स्तरीय एकीकृत पोर्टल—टिकट-नंबर, टाइम-स्टैम्प, SLA, और ऑटो-SMS/ईमेल अपडेट। डेटा-थ्रू-ओपन API से जिला-वार प्रदर्शन रैंकिंग।
7. एविडेंस संरक्षण: पोस्ट-मार्टम की वीडियोग्राफी अनिवार्य, शरीर-चोट फ़ोटो-मैट्रिक्स, बॉडी-कैम/डैश-कैम का 100% रोल-आउट, और चेन-ऑफ-कस्टडी SOP।
8. प्रशिक्षण व संस्कृति: SC/ST अत्याचार, जेंडर-संवेदनशीलता, मीडिया/शिकायतकर्ता-इंटरफ़ेस, और कम्युनिटी-पोलिसिंग के लिए निरंतर प्रशिक्षण; ग्रिवांस-डेज़ (जैसे 'वादी संवाद दिवस') का साप्ताहिक संस्थानीकरण।
(D) सामाजिक/नागरिक
9. व्हिसलब्लोअर व गवाह-सुरक्षा: सख़्त रिटालिएशन-रोधी प्रोटोकॉल; शिकायतकर्ता/पत्रकारों के लिए फास्ट-ट्रैक नॉन-कॉग्निजेबल-टू-कॉग्निजेबल रिव्यू और समन्वित विटनेस-प्रोटेक्शन स्कीम।
10. पारदर्शिता व मीडिया: जिला-वार एन्काउंटर/हिरासत-मृत्यु डैशबोर्ड; मीडिया-ब्रिफिंग में FIR-नंबर, जाँच-एजेंसी, पोस्ट-मार्टम/वीडियो-लिंक; RTI-उन्मुख प्रो-एक्टिव डिस्क्लोज़र।
उत्तर प्रदेश-केंद्रित 10-बिंदु कार्ययोजना (12 महीनों में)
1. सभी थानों में e-FIR/Zero-FIR के SOP जारी 3 दिन में ई-सिग्नेचर/कन्फर्मेशन, 24 घंटे में FIR-कॉपी।
2. PUCL अनुपालन: हर मुठभेड़-मृत्यु पर स्वत: FIR + स्वतंत्र SIT; 90 दिनों में मजिस्ट्रियल रिपोर्ट सार्वजनिक।
3. Paramvir Singh के तहत CCTV + ऑडियो 100% कवरेज; डिस्ट्रिक्ट-ओवरसाइट कमेटी की मासिक रिपोर्टें वेबसाइट पर।
4. जिला-स्तरीय PCA को स्वतंत्र स्टाफ/बजट/समन-शक्ति; सिफ़ारिशों पर टाइम-बाउंड अनुशासनात्मक कार्रवाई।
5. NHRC 24-घंटे रिपोर्टिंग व पोस्ट-मार्टम-वीडियोग्राफी का जिला-वार अनुपालन सूचकांक, अनुपालन न होने पर SP/DM की जवाबदेही।
6. हिरासत-स्वास्थ्य प्रोटोकॉल: मेडिकल स्क्रीनिंग, दवा/बीमारी-लॉग, परिवार/वकील को SMS-अलर्ट; हर डिटेनी को 24×7 लीगल-ऐड हेल्पलाइन।
7. समुदाय-संवाद: 'वादी संवाद दिवस' जैसे साप्ताहिक संवाद का राज्य-व्यापी विस्तार; लंबित FIR/जाँच की सार्वजनिक क्लोजर-पंक्ति।
8. संवेदनशील मामलों का एसओपी: महिलाओं/SC-ST/पत्रकार-कार्यकर्ताओं की शिकायतों के लिए गजेटेड ऑफ़िसर-लीड सेल, 72-घंटे में एक्शन रिपोर्ट।
9. डेटा-पारदर्शिता: एन्काउंटर/कस्टोडियल-डेथ के माइक्रोडेटा (तारीख, स्थान, जाँच-एजेंसी, स्टेटस) को ओपन-डेटासेट के रूप में प्रकाशित।
10. प्रोत्साहन व दंड: थानों/जिलों के लिए जवाबदेही-स्कोर; शीर्ष 10 को प्रोत्साहन, न्यूनतम स्कोर वालों पर परफॉर्मेंस-इम्प्रूवमेंट प्लान।
समस्या किसी एक कड़ी में नहीं, बल्कि पूरी शृंखला FIR से लेकर हिरासत, जाँच, फॉरेंसिक, निगरानी, अभियोजन और सार्वजनिक पारदर्शिता में फैली है। अच्छी ख़बर यह है कि कानूनी कसौटियाँ Lalita Kumari, D.K. Basu, PUCL, Paramvir Singh, Prakash Singh स्पष्ट हैं; BNSS-2023 ने डिजिटल/ज़ीरो-FIR से इनको और क्रियाशील बनाने का औज़ार दिया है। अब आवश्यकता है राजनीतिक-प्रशासनिक इच्छाशक्ति, स्वतंत्र निगरानी संस्थाएँ जिनके पास दंत-नख हों, और पब्लिक-फेसिंग पारदर्शिता जिससे व्यवस्था जनता को समझाने नहीं, सबूत दिखाने लगे। यही रास्ता है जिससे उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग कानून के राज और मानव-अधिकार-सम्मान की ओर निर्णायक मोड़ ले सकती है।
What's Your Reaction?