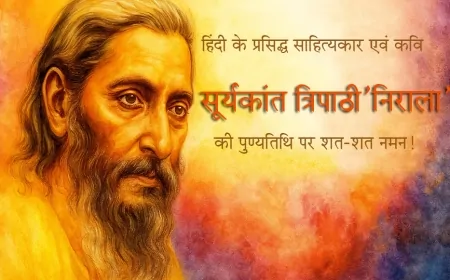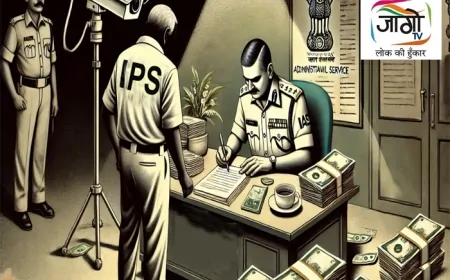शिक्षक दिवस 2025: शिक्षा और शिक्षक की बदलती भूमिका पर नई दृष्टि
5 सितम्बर, शिक्षक दिवस पर डॉ. राधाकृष्णन की विरासत के साथ आज की शिक्षा व्यवस्था पर विमर्श। नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, शैक्षणिक असमानताएँ, बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य और बाजारीकरण जैसी चुनौतियों के बीच शिक्षक की भूमिका और भविष्य की दिशा पर गहन संपादकीय।
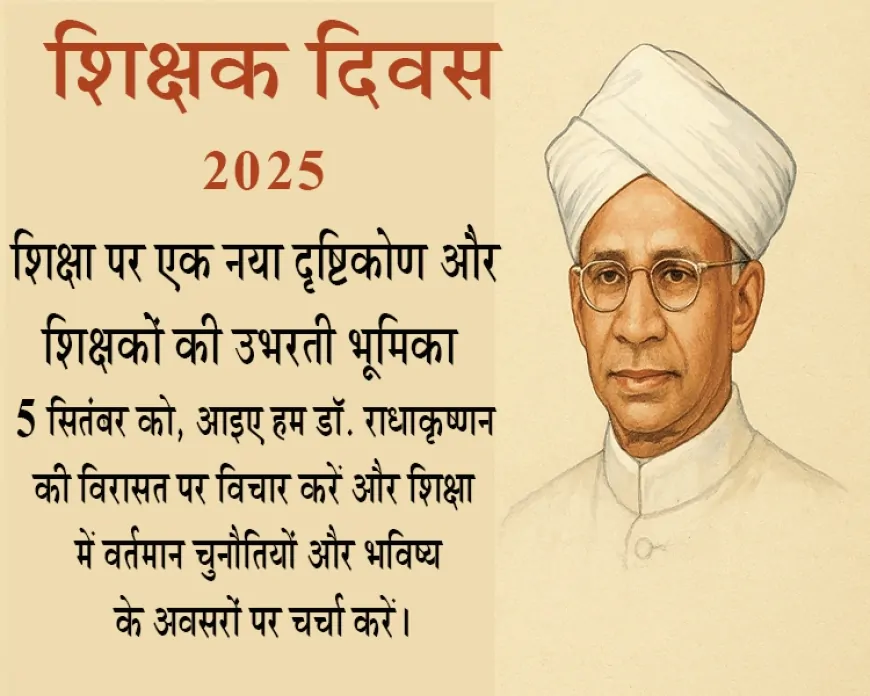
शिक्षक दिवस: शिक्षा और शिक्षक की बदलती भूमिका पर पुनर्विचार
भारत में हर वर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महज़ एक औपचारिक उत्सव नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस शाश्वत सत्य का स्मरण है कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इस दिन हम स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनयिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हैं। जब उनके शिष्यों ने उनके जन्मदिवस को मनाने की इच्छा व्यक्त की थी, तब उन्होंने स्वयं कहा था, “यदि आप सचमुच मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए।” यह कथन ही शिक्षा और शिक्षक की सर्वोच्चता का प्रमाण है।
परंतु इस श्रद्धांजलि के साथ ही यह दिन हमें यह सोचने का अवसर भी देता है कि शिक्षा का वर्तमान स्वरूप क्या है, उसकी चुनौतियाँ कहाँ हैं, और भविष्य की दिशा कैसी होनी चाहिए।
आज की शिक्षा-व्यवस्था: नई संभावनाएँ और प्रश्न
21वीं सदी में शिक्षा केवल कक्षाओं और ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रही। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) ने शिक्षा को व्यापक दृष्टि दी है। इसमें समग्रता, लचीलापन, बहुभाषिकता, कौशल-आधारित शिक्षा और अनुसंधान पर ज़ोर दिया गया है। पहली बार यह मान्यता मिली कि शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन कौशल और रचनात्मकता का विकास भी करे।
डिजिटल शिक्षा ने इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने शिक्षा को भौगोलिक सीमाओं से परे पहुँचाया है। ऑनलाइन-हाइब्रिड मॉडल ने महामारी के समय शिक्षा को टिकाए रखा। वर्चुअल क्लासरूम, एआई-सहायक सामग्री, और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ (OER) ने सीखने के नए अवसर दिए।
लेकिन, साथ ही यह प्रश्न भी उठता है, क्या तकनीक शिक्षा को सबके लिए समान रूप से सुलभ बना रही है, या उसने नई असमानताएँ पैदा कर दी हैं?
बदलते समय में शिक्षक की भूमिका
शिक्षक अब केवल ज्ञान-संप्रेषक नहीं हैं, बल्कि मार्गदर्शक, सहयात्री और प्रेरक भी हैं। आज का छात्र इंटरनेट पर अनगिनत जानकारियाँ पा सकता है। ऐसे में शिक्षक का कार्य केवल तथ्य बताना नहीं, बल्कि उस जानकारी को परखने की क्षमता, आलोचनात्मक दृष्टि और नैतिक मूल्यों से जोड़ना है।
नई शिक्षा नीति भी यह अपेक्षा करती है कि शिक्षक अनुसंधान-उन्मुख हों, शिक्षा को अनुभवात्मक बनाएँ और विद्यार्थियों में रचनात्मकता व समस्या-समाधान क्षमता विकसित करें।
आज का शिक्षक तभी सफल है जब वह तकनीक को अपनाते हुए भी मानवीय संवाद को केंद्र में रखे। क्योंकि शिक्षा केवल स्क्रीन पर लिखे शब्दों से नहीं, बल्कि शिक्षक की संवेदनशील दृष्टि और जीवनानुभव से जीवंत होती है।
शैक्षणिक असमानताएँ: सबसे बड़ी बाधा
भारतीय शिक्षा-व्यवस्था की सबसे गंभीर चुनौती है, असमानता।
ग्रामीण बनाम शहरी अंतर: शहरों में आधुनिक स्कूल, तकनीकी साधन और प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जबकि गाँवों में आज भी बुनियादी ढाँचे की कमी है।
डिजिटल डिवाइड: महामारी के दौरान लाखों छात्रों के पास स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप या स्थायी इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। परिणामस्वरूप उनकी पढ़ाई बाधित हो गई।
सरकारी बनाम निजी स्कूल: जहाँ निजी विद्यालय वैश्विक स्तर की सुविधाएँ प्रदान करने का दावा करते हैं, वहीं सरकारी विद्यालय संसाधनों और शिक्षकों की कमी से जूझते रहते हैं। यदि शिक्षा का अधिकार वास्तव में सबके लिए है, तो इन खाइयों को पाटना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
समसामयिक चुनौतियाँ
शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं है, वह पूरे समाज की धड़कनों से जुड़ी है। आज की प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
बेरोजगारी: लाखों डिग्रीधारी युवा नौकरी के अभाव में निराश हैं। यह प्रश्न उठता है—क्या शिक्षा केवल रोजगार दिलाने का साधन है, या जीवन को सार्थक बनाने का भी मार्ग है?
शिक्षा का बाजारीकरण: शिक्षा संस्थान आज 'कॉर्पोरेट' मॉडल पर चल रहे हैं। फीस, कोचिंग कल्चर और डिग्री का व्यापार छात्रों को ग्राहक बना देता है।
परीक्षा-प्रणाली: रटंत पद्धति और बोर्ड/प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव बच्चों की सृजनात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुँचा रहा है।
मानसिक स्वास्थ्य: अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसे मामले छात्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं। शिक्षकों पर भी लक्ष्य और परिणाम देने का दबाव अस्वाभाविक रूप से बढ़ गया है।
भविष्य की दिशा: शिक्षक की केंद्रीय भूमिका
भविष्य का भारत तभी सशक्त होगा जब उसके शिक्षक आने वाली पीढ़ी में संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक मूल्य और पर्यावरणीय चेतना का बीज रोपें।
सामाजिक संवेदनशीलता: छात्र केवल अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर या वकील न बनें, बल्कि अच्छे नागरिक और संवेदनशील इंसान भी बनें।
लोकतांत्रिक मूल्य: संवाद, बहस, मतभिन्नता का सम्मान ये गुण शिक्षा के जरिए ही विकसित हो सकते हैं।
पर्यावरणीय चेतना: जलवायु संकट के दौर में शिक्षा को पर्यावरण की रक्षा को जीवन का हिस्सा बनाना होगा।
कौशल आधारित शिक्षा: 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में डिजिटल, व्यावसायिक और उद्यमिता कौशल आवश्यक हैं। शिक्षक इनका मार्गदर्शन करेंगे।
प्रेरणा का भाव
शिक्षक दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का अवसर भी है। डॉ. राधाकृष्णन मानते थे कि “सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को स्वतंत्र विचार, सहिष्णुता और नैतिकता की ओर ले जाए।” आज जब दुनिया तेज़ बदलावों, बाजारीकरण और तकनीकी उथल-पुथल से गुज़र रही है, तब शिक्षक ही वह धुरी हैं जो विद्यार्थियों को संतुलन, मानवीयता और विवेक सिखा सकते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षक केवल कक्षा तक सीमित नहीं होते, वे समाज निर्माता हैं।
शिक्षक दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम शिक्षा और शिक्षकों को किस दृष्टि से देखते हैं। यदि हम केवल परीक्षा परिणाम, नौकरी और वेतन को शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मानेंगे, तो हम शिक्षा के मूल दर्शन से भटक जाएँगे। लेकिन यदि हम इसे मानवता, समानता और रचनात्मकता का मार्ग मानेंगे, तो हम एक सशक्त, संवेदनशील और समृद्ध समाज की ओर बढ़ेंगे। आज का शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं, बल्कि युगद्रष्टा है। उसकी भूमिका है भविष्य की पीढ़ियों को वह दृष्टि देना, जो उन्हें न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी ज़िम्मेदार बनाए। शिक्षक दिवस पर हमें प्रण करना चाहिए कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि शिक्षा को अधिक न्यायसंगत, मानवीय और सुलभ बनाकर करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
What's Your Reaction?