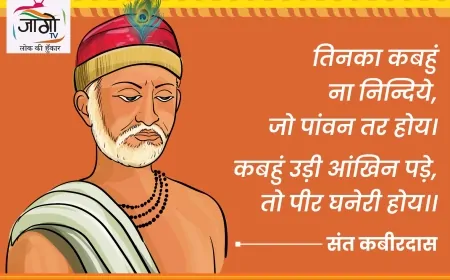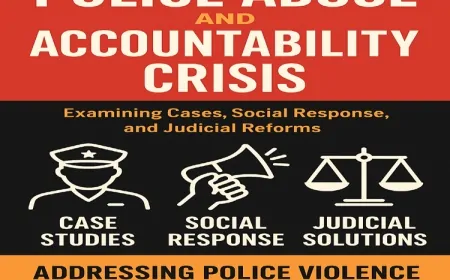शारीरिक स्वायत्तता: स्वतंत्रता से संविधान तक एक सामाजिक, नैतिक और नीतिगत विमर्श
शारीरिक स्वायत्तता केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, बल्कि यह स्वास्थ्य, गरिमा, लैंगिक समानता और मानवाधिकारों की बुनियाद है। भारत में महिलाओं, LGBTQ+ समुदाय, किशोरों और यौन हिंसा के पीड़ितों के संदर्भ में यह अधिकार बार-बार सामाजिक, धार्मिक और कानूनी नियंत्रणों से बाधित होता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों को अपने शरीर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। इसके लिए कानूनों, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सोच में व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि हर नागरिक को सम्मानपूर्वक और स्वायत्त जीवन जीने का अवसर मिल सके।
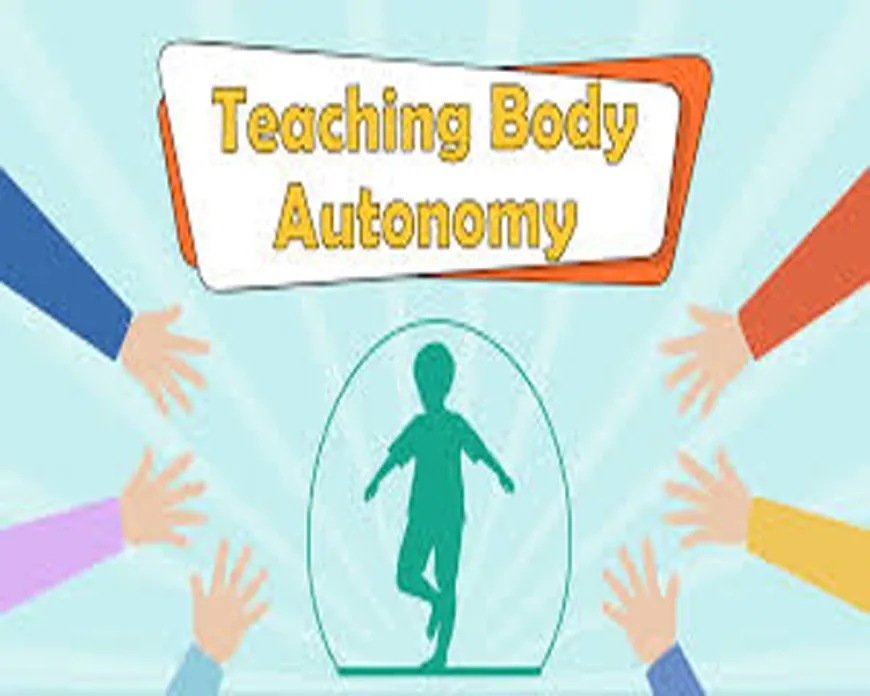
'मेरे शरीर पर मेरा अधिकार' कोई नारा मात्र नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र के सबसे बुनियादी मूल्य स्वतंत्रता, गरिमा और समानता का घोष है।
1. शारीरिक स्वायत्तता: परिभाषा और व्यापक महत्व
शारीरिक स्वायत्तता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार हो — चाहे वह यौन संबंधों, स्वास्थ्य सेवाओं, गर्भधारण या गर्भपात जैसे मुद्दों पर हो। यह अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं करता, बल्कि यह स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरिमा और मानवाधिकारों की बुनियाद है।
UNFPA (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) के अनुसार, शारीरिक स्वायत्तता का हनन दुनिया भर में एक व्यापक और गहन समस्या है और भारत कोई अपवाद नहीं है।
2. सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोध: पितृसत्ता और नियंत्रण की जड़ें
भारतीय समाज की संरचना अभी भी गहराई से पितृसत्तात्मक है, जहाँ महिलाएँ , LGBTQ+ व्यक्ति, किशोर और यौन हिंसा के पीड़ित अपने शरीर पर नियंत्रण से वंचित कर दिए जाते हैं।
पारिवारिक और धार्मिक नियंत्रण: विवाह, यौन संबंध और प्रजनन के बारे में निर्णय अक्सर परिवार, समाज या धार्मिक संस्थाएँ लेती हैं, न कि स्वयं व्यक्ति।
कौमार्य, इज्जत और संस्कृति: महिला की स्वतंत्रता को 'घर की इज्जत' से जोड़ कर देखा जाता है।
LGBTQ+ के अस्तित्व पर ही सवाल: 377 हटने के बावजूद समाज में समलैंगिक संबंधों, ट्रांसजेंडर अधिकारों और पहचान को लेकर व्यापक भेदभाव और हिंसा जारी है।
3. भारत में कानूनी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य की स्थिति
कानूनी पहलू:
MTP Act (2021): संशोधित गर्भपात कानून ने कुछ सुधार लाए हैं, लेकिन महिलाओं को'डॉक्टरी सहमति” की बाध्यता अभी भी उनके आत्मनिर्णय को सीमित करती है।
POCSO Act: किशोरियों की यौन गतिविधियों को आपराधिक मानना, उनके शरीर और इच्छाओं को ‘न्याय व्यवस्था’ द्वारा नकारने जैसा है।
Section 377 का निष्कासन (2018): LGBTQ+ अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर, लेकिन विधिक संरचना अभी भी समावेशी नहीं है (उदाहरण: विवाह, गोद लेने का अधिकार)।
Transgender Persons Act (2019): पहचान और अधिकार देने का प्रयास, लेकिन इसका क्रियान्वयन कमजोर है और आलोचना का शिकार रहा है।
सामाजिक सच्चाई:
NFHS-5 (2019–21) के अनुसार:
केवल 55% महिलाएँ ही अपनी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों का निर्णय स्वयं लेती हैं।
किशोर गर्भधारण और गर्भपात तक पहुँच में भारी क्षेत्रीय असमानता है।
LGBTQ+ समुदाय: आत्महत्या दरें ऊँची, स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव और सामाजिक तिरस्कार आम है।
रिपोर्टेड रेप मामलों में भी पीड़ितों की मेडिकल काउंसलिंग और कानूनी सहायता सीमित होती है।
4. शारीरिक स्वायत्तता: एक नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार की गारंटी देते हैं। लेकिन, इस गारंटी को व्यावहारिक रूप देने के लिए यह ज़रूरी है कि:
राज्य सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के स्वास्थ्य, जानकारी और निर्णय की स्वतंत्रता प्रदान करे।
कानून केवल अपराध को नहीं, बल्कि मानव गरिमा की रक्षा को प्राथमिकता दें।
5. समाधान की दिशा: एक समग्र सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण
कानूनी सुधार:
गर्भपात, यौन पहचान, और किशोर स्वास्थ्य के संदर्भ में सहमति और आत्मनिर्णय को केंद्रीय मान्यता देना।
LGBTQ+ विवाह, संपत्ति अधिकार, मेडिकल निर्णय आदि को कानूनी संरक्षण देना।
शिक्षा और जनसंवाद:
यौन शिक्षा (Comprehensive Sexuality Education) को स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य करना।
मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों के ज़रिए बॉडी ऑटोनॉमी पर जनजागरूकता फैलाना।
स्वास्थ्य नीति सुधार:
यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ हर वर्ग, खासकर महिलाओं, ट्रांसजेंडर और किशोरों के लिए सुलभ और गोपनीय हों।
मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग सेवाओं का विस्तार किया जाए।
सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन:
परिवार, धार्मिक संस्थाएँ , और सामुदायिक नेतृत्व को प्रगतिशील संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षित करना।
'इज्जत' की आड़ में महिला और यौन अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को दबाना अपराध और नैतिक विफलता दोनों समझा जाए।
शारीरिक स्वायत्तता सिर्फ एक व्यक्तिगत माँग नहीं, बल्कि यह उस समाज और राष्ट्र के चरित्र की पहचान है जो अपने नागरिकों को गरिमा, समानता और स्वतंत्रता देता है। भारत में यह अधिकार न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि LGBTQ+ समुदाय, यौन हिंसा पीड़ितों और युवाओं के लिए जीवन और न्याय का मूल आधार बन गया है। आज जब नीति-निर्माण, शिक्षा और समाज के स्तर पर संवेदनशील बदलाव की ज़रूरत है, तब शारीरिक स्वायत्तता को केवल मानवाधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्र की संवैधानिक आत्मा के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य है।
What's Your Reaction?