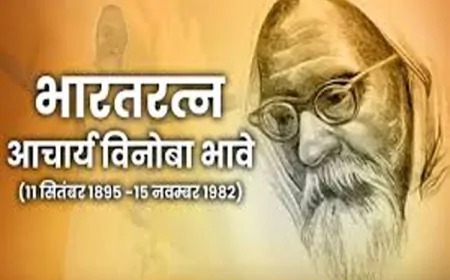‘स्वराज’ से राष्ट्र-बोध तक: लोकमान्य तिलक के विचारों की आज के भारत में प्रासंगिकता
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों में से एक थे, बल्कि उन्होंने भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक नवजागरण की नींव रखी। ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है’ जैसा घोषवाक्य केवल राजनीतिक क्रांति का उद्घोष नहीं था, बल्कि भारतीय चेतना के पुनरुत्थान का बिगुल था। तिलक का राजनीतिक दर्शन, उनकी पत्रकारिता, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान, और धर्म को राष्ट्रनिर्माण का माध्यम बनाने की उनकी सोच इन सबने एक ऐसे भारत की कल्पना प्रस्तुत की जो आत्मनिर्भर, आत्मगौरव से पूर्ण और संगठित हो। यह लेख तिलक के विचारों को समकालीन भारत के लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में विश्लेषित करता है, और यह विवेचना करता है कि तिलक आज भी क्यों एक प्रासंगिक वैचारिक प्रेरणा बने हुए हैं।
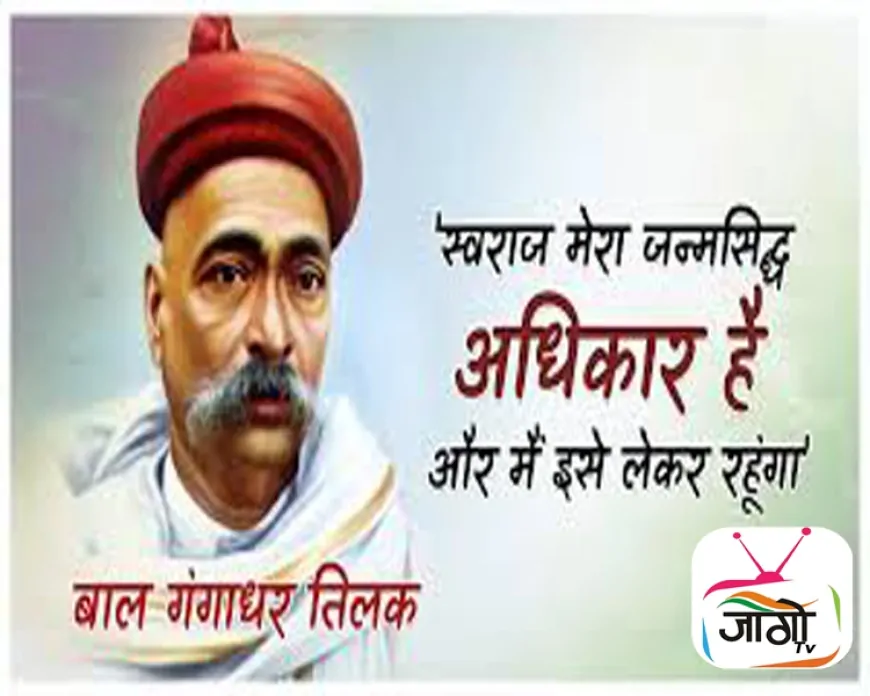
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों में से एक थे, बल्कि उन्होंने भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक नवजागरण की नींव रखी। ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है’ जैसा घोषवाक्य केवल राजनीतिक क्रांति का उद्घोष नहीं था, बल्कि भारतीय चेतना के पुनरुत्थान का बिगुल था। तिलक का राजनीतिक दर्शन, उनकी पत्रकारिता, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान, और धर्म को राष्ट्रनिर्माण का माध्यम बनाने की उनकी सोच इन सबने एक ऐसे भारत की कल्पना प्रस्तुत की जो आत्मनिर्भर, आत्मगौरव से पूर्ण और संगठित हो।
1. ‘स्वराज’ की अवधारणा: आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का सूत्र
बाल गंगाधर तिलक ने ‘स्वराज’ को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए यह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आत्मगौरव, सांस्कृतिक स्वाभिमान, और नैतिक आत्मनिर्भरता का पर्याय था। तिलक ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति की माँग केवल इसलिए नहीं की कि वह विदेशी था, बल्कि इसलिए कि वह भारतीयों को अधीन नागरिक बनाकर उन्हें नैतिक और सांस्कृतिक रूप से भीन कर रहा था।
2. गरम दल का वैचारिक आधार: नरमपंथियों से अलग दृष्टिकोण
जहाँ एक ओर गोखले जैसे नरमपंथी नेता संवैधानिक सुधारों और संवाद की बात करते थे, वहीं तिलक का मानना था कि दमन के सामने प्रतिरोध और आत्मबल आवश्यक है। उनका राष्ट्रवाद सक्रिय, आत्माभिमानी और जनसंपृक्त था।
3. पत्रकारिता: केसरी और मराठा के माध्यम से जनचेतना का विस्तार
तिलक ने 'केसरी' (मराठी) और 'मराठा' (अंग्रेज़ी) जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जनमत निर्माण को एक क्रांतिकारी हथियार बनाया। ब्रिटिश शासन के दमन के बावजूद उन्होंने लेखनी को कभी न रोका। प्रेस को उन्होंने केवल समाचार का माध्यम नहीं, बल्कि जनजागरण और प्रतिरोध की राजनीति का मंच बनाया।
4. शिक्षा और संस्कृति: स्वतंत्रता की बुनियाद
तिलक का विश्वास था कि गुलामी की सबसे बड़ी जड़ मानसिक दासता है। उन्होंने भारतीय इतिहास, गणित, ज्योतिष और वेदों की प्रतिष्ठा को पुनःस्थापित करने का प्रयास किया। वे अंग्रेजी शिक्षा के एकतरफा वर्चस्व के विरोधी थे और स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था के समर्थक।
5. गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव: सांस्कृतिक एकता और राजनीतिक उद्देश्य
तिलक ने लोकआस्था से जुड़े उत्सवों को सामूहिक चेतना और राजनीतिक जागरूकता का माध्यम बनाया।
गणेशोत्सव को सार्वजनिक मंच बनाकर हिंदू-मुस्लिम एकता और संगठन का संदेश दिया।
शिवाजी उत्सव के माध्यम से उन्होंने ऐतिहासिक प्रेरणा को जनमानस से जोड़ा।
यह रणनीति आज भी प्रासंगिक है, बशर्ते इसका उपयोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बजाय सांस्कृतिक एकता के लिए हो।
6. ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आत्मबल और वैचारिक असहमति
तिलक का विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए वैचारिक निर्भीकता अनिवार्य है। वे सत्ता से टकराने से कभी नहीं डरे। उन्होंने कहा था: "यदि मैं जेल जाता हूँ, तो वह भी मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि वह देश के लिए है।" उनका यह दृष्टिकोण आज भी असहमति के अधिकार और वैकल्पिक विचार की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा है।
7. तिलक का विचार आज क्यों प्रासंगिक है?
राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रहित:
आज जब राष्ट्रवाद का प्रयोग अक्सर विभाजनकारी नारों और हिंसक विमर्शों में हो रहा है, तिलक का समावेशी और चेतनासंपन्न राष्ट्रवाद एक संयमित विकल्प प्रस्तुत करता है। उनका राष्ट्रवाद सभ्यता, संस्कृति और स्वाभिमान से उपजा था, न कि नफ़रत और वर्चस्व की भावना से।
धर्मनिरपेक्षता और सार्वजनिक धर्म का संतुलन:
तिलक ने धर्म को सामाजिक चेतना के रूप में देखा, न कि राजनीतिक उपकरण के रूप में। आज जब धर्म आधारित राजनीति समाज को विभाजित कर रही है, तिलक का मॉडल धर्म-संस्कृति को एकता और प्रेरणा का साधन बनाने की बात करता है।
नागरिक अधिकार और कर्तव्य का संतुलन:
आज के भारत में नागरिक अधिकारों की चर्चा तो होती है, पर तिलक की तरह कर्तव्यों की चेतना नहीं है। उन्होंने नागरिक को न केवल हक माँगने वाला, बल्कि राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में देखा।
युवाओं के लिए वैचारिक प्रेरणा:
आज के युवाओं को तिलक से यह सीखना चाहिए कि विचार, संगठन, शिक्षा और आत्मबल के ज़रिए भी क्रांति लाई जा सकती है। तिलक ‘गति’ और ‘दिशा’ दोनों देते हैं जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है।
लोकमान्य तिलक केवल स्वतंत्रता आंदोलन के नेता नहीं थे, वे भारत की राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक आत्मा और सामाजिक संगठन के सूत्रधार भी थे। आज जब लोकतंत्र को नई चुनौतियाँ मिल रही हैं- ध्रुवीकरण, असहमति का दमन, और नैतिक गिरावट तब तिलक का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि स्वराज केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि आत्मबल, शिक्षा, संस्कृति और नागरिक जिम्मेदारी का समुच्चय है।
What's Your Reaction?