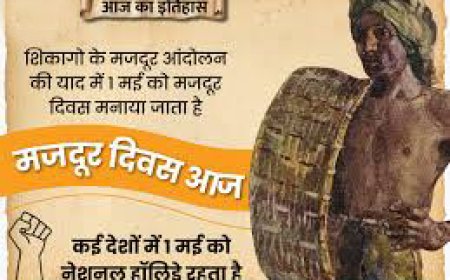भारत में फर्जी एनकाउंटर क्यों बढ़े? आंकड़े, केस स्टडी और पुलिस सुधार की जरूरत
भारत में फर्जी एनकाउंटर और पुलिस मनमानी क्यों बढ़ रही है? NHRC रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, यूपी-बिहार-पंजाब के केस स्टडी, जातीय पूर्वाग्रह और न्यायिक खामियों पर विश्लेषण। पढ़ें पूरा लेख।
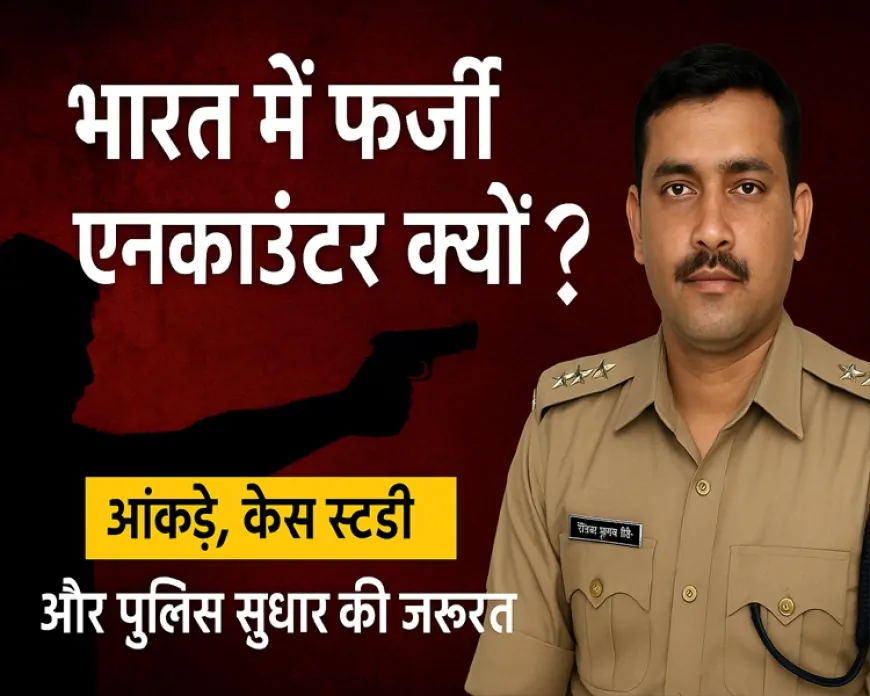
भारत का लोकतंत्र संविधान, क़ानून और न्यायिक प्रक्रिया पर आधारित है। लेकिन, हाल के वर्षों में पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर, जातीय पूर्वाग्रह और आम नागरिकों पर गोलीबारी की घटनाओं ने गंभीर चिंता पैदा की है। ऐसे मामले केवल अपराध नियंत्रण या 'तत्काल न्याय' के बहाने नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास और नागरिक अधिकारों पर हमला भी हैं।
सरकारी डेटा और ट्रेंड विश्लेषण
गृह मंत्रालय के अनुसार, 2016 से 2022 के बीच पुलिस मुठभेड़ों में 655 मौतें दर्ज हुईं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 2017-18 से 2021-22 के बीच पुलिस मुठभेड़ों पर 813 शिकायतें प्राप्त कीं। इनमें से अधिकांश मामलों में न्यायिक जाँच लंबित है।
राज्यवार ट्रेंड
उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 के बीच 150+ कथित एनकाउंटर मौतें हुईं।
छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश में नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज हुईं।
पंजाब और बिहार में राजनीतिक रूप से चर्चित 'फेक एनकाउंटर केस' लंबे समय से विवादित हैं।
सुप्रीम कोर्ट (People’s Union for Civil Liberties बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2014) ने स्पष्ट कहा कि हर एनकाउंटर की न्यायिक जाँच अनिवार्य है और FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन, राज्यों में इस गाइडलाइन का पालन आंशिक ही हुआ।
जाति, वर्ग और सामाजिक कोण
फर्जी एनकाउंटर केवल 'कानून-व्यवस्था' की समस्या नहीं हैं, बल्कि अक्सर वे सामाजिक असमानता और जातीय पूर्वाग्रह का प्रतिबिंब बनते हैं।
दलित और आदिवासी समुदाय disproportionate तौर पर पीड़ित पाए गए हैं। NHRC की 2020 रिपोर्ट में कहा गया कि आदिवासी इलाकों में मुठभेड़ों को 'नक्सल विरोधी अभियान' का नाम देकर वैध ठहराया जाता है।
अल्पसंख्यक समुदायों पर 'आतंकवाद' या 'गैंगस्टर' टैग लगाकर मनमाने ढंग से एनकाउंटर किए जाने के आरोप लगते रहे हैं।
इसका शिकार केवल गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित तबका ही नहीं होता है, बल्कि इसका शिकार वह भी होते हैं जो पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, जिनके पास संवैधानिक समझ भी होती है, राजनीतिक पहुँच भी होती है, जो कानूनी लड़ाई लड़ने की क्षमता भी रखते हैं वह भी पुलिस का सबसे आसान शिकार बनते हैं। ज्यादातर पुलिसकर्मी अपने विभाग के भ्रष्ट, विधि की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को बचाने के लिए वे पीड़ित परिवार की हत्या तक करवाने से भी नहीं चूकते हैं, इसमें DSP लेवल से लेकर उपायुक्त स्तर के अधिकारी तो बड़े सहजता से यह कार्य करते हैं। इनके कार्यों से तो यह साफ-साफ खुली आँखों से दिख जाता है कि इन्हें जो तनख्वाह मिलती है सिर्फ इसी कार्य के लिए मिलती है।
पुलिस जाँच और न्यायिक प्रक्रिया की खामियाँ
अधिकांश मामलों में FIR पुलिस ही पुलिसकर्मियों पर दर्ज करती है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
जाँच एजेंसी वही पुलिस बल होती है, जिससे 'conflict of interest' पैदा होता है।
गवाहों की सुरक्षा नहीं होने के कारण परिवार अक्सर बयान बदलने या चुप रहने को मजबूर हो जाते हैं।
फर्जी मुकदमों में न्यायिक प्रक्रिया लंबी खिंचती है। NCRB के अनुसार, 2019 में दर्ज पुलिस अत्याचार के मामलों में सजा दर केवल 2.5% रही।
पीड़ित परिवारों की स्थिति और सरकारी प्रतिक्रिया
लकी तिवारी (BIHAR, 2025), बिहार के मुजफ्फरपुर के मनोज यादव एनकाउंटर केस, और पंजाब में 1990 के दशक के 'counter-insurgency operations' में परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं।
NHRC ने कई मामलों में मुआवज़े की सिफारिश की, लेकिन लंबे न्यायिक विलंब और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पीड़ित परिवार आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट से जूझते हैं। कई परिवार तो पुलिस के डर से सार्वजनिक बयान भी नहीं दे पाते।
केस स्टडी
(i) लकी तिवारी केस, बिहार (2025)
पुलिस ने उसे 'कुख्यात अपराधी' बताया, जबकि स्थानीय एवं परिवारजनों का कहना है कि उस पर कोई मौजूदा आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। लकी तिवारी के बयान अनुसार, वह अपनी माँ के लिए फल खरीदने गया था और पुलिस की दो गाड़ियों ने घेरकर दोनों पैरों में गोली मार दी। पुलिस अधिकारियों ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है; मामला जाँचाधीन है।
(ii) सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर, गुजरात (2005)
इस केस ने राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचाया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जाँच हुई, कई वरिष्ठ IPS अधिकारी आरोपी बने। लेकिन, गवाहों के पलट जाने और लंबी सुनवाई के बाद अधिकांश आरोपी बरी हो गए।
(iii) मनोज यादव केस, बिहार (2017)
एक गरीब किसान परिवार से आए मनोज यादव को 'माओवादी सहयोगी' बताकर पुलिस ने गोली मार दी। बाद में साबित हुआ कि वह निर्दोष था। लेकिन परिवार को केवल आंशिक मुआवजा और कोई न्याय नहीं मिला।
(iv) पंजाब के 'फर्जी एनकाउंटर' (1984–1995)
आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान हजारों युवकों को 'लॉ एंड ऑर्डर' के नाम पर गायब या मार दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों को सुनवाई के लिए पुनः खोला। परंतु अधिकांश परिवार अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मीडिया और समाज की भूमिका
सबसे बड़ा दिवालियापन मीडिया में है। जिसमें कुछ चैनल पुलिस को 'हीरो' बताकर एनकाउंटर को 'तत्काल न्याय' के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे दुखद स्थिति एक लोकतांत्रिक गणराज्य में और कुछ हो ही नहीं सकता।
वहीं, खोजी पत्रकारिता ने कई फर्जी एनकाउंटरों का पर्दाफाश भी किया (जैसे सोहराबुद्दीन केस, मणिपुर एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग्स पर Tehelka की रिपोर्टिंग)।
सुधार और सुझाव
1. स्वतंत्र जाँच एजेंसी – हर एनकाउंटर केस की जाँच CBI या न्यायिक आयोग से हो।
2. बॉडी कैमरा और CCTV – मुठभेड़ ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो।
3. गवाह संरक्षण कार्यक्रम – ताकि परिवार और चश्मदीद सुरक्षित रह सकें।
4. पुलिस प्रशिक्षण और संवेदनशीलता – जातीय/सामाजिक पूर्वाग्रह को कम करने के लिए नियमित प्रशिक्षण।
5. मीडिया की जवाबदेही – बिना तथ्यों की पुष्टि 'एनकाउंटर स्टोरी' को sensationalize करने पर रोक।
6. कानूनी सुधार – सुप्रीम कोर्ट की 2014 गाइडलाइन को सभी राज्यों में कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए।
नीति और नैतिकता का सवाल
फर्जी एनकाउंटर केवल क़ानून और न्याय का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को आहत करने वाली प्रवृत्ति है। जब राज्य स्वयं 'कानून के बाहर' खड़ा हो जाए, तो नागरिकों का विश्वास टूटता है। भारत की पुलिस व्यवस्था को लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकार और संवैधानिक जिम्मेदारियों के अनुरूप ढालना अब नितांत आवश्यक है। न्याय में देर हो सकती है, परन्तु उसे त्वरित हिंसा या जातीय पूर्वाग्रह से प्रतिस्थापित करना समाज और राज्य – दोनों के लिए घातक है।
What's Your Reaction?