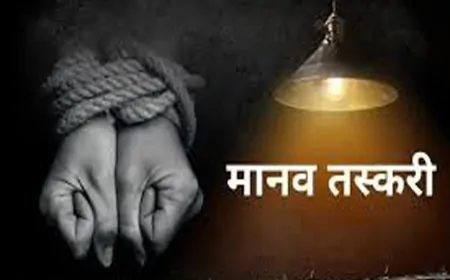कबीर: भक्ति, बोध और बदलाव के महाकवि
15वीं शताब्दी के धार्मिक उन्माद, जातीय भेद और पाखंड के विरुद्ध कबीर ने अपने निर्भीक विचारों से क्रांति की मशाल जलाई। उन्होंने निर्गुण भक्ति को आधार बनाकर धर्म के आडंबर, जातिवाद और मूर्तिपूजा के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। यह लेख कबीर को एक समाज-सुधारक, एक भक्ति आंदोलक और एक ऐसे संत के रूप में स्थापित करता है जिन्होंने धार्मिक समरसता की नींव रखी। साथ ही यह लेख बताता है कि आज के खंडित सामाजिक-सांप्रदायिक परिदृश्य में कबीर का चिंतन कितना प्रासंगिक है।
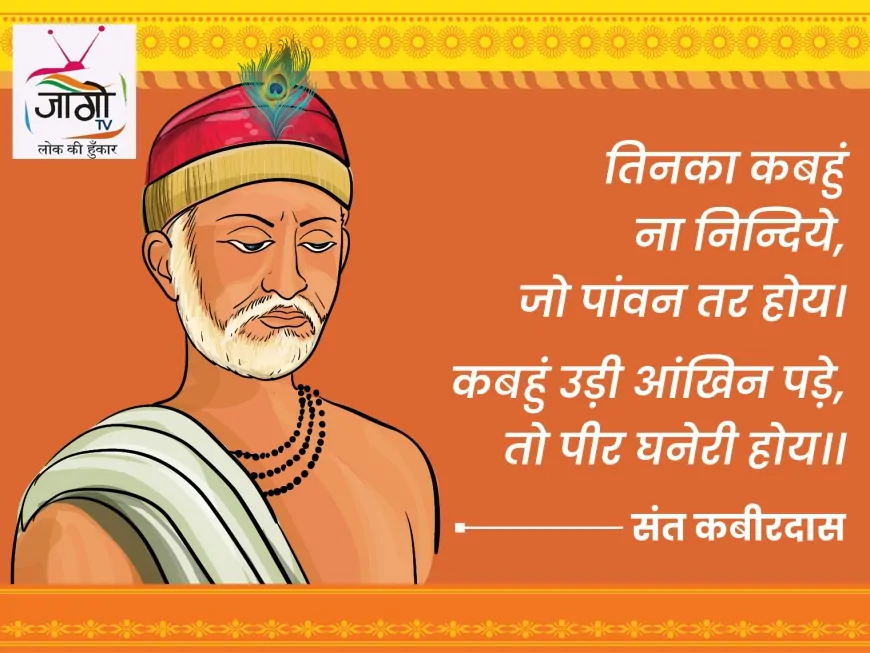
भारतीय जनमानस में यदि कोई ऐसा संत हुआ है जिसने धर्म की रूढ़ियों को तोड़ते हुए, आत्मा के मुक्त स्वरूप की घोषणा की हो, तो वह हैं संत कबीर। वे न तो परंपरागत संत थे, न ब्राह्मणीय व्यवस्था के पोषक और न ही किसी एक धर्म के अनुयायी। वे उस युग की ज़रूरत थे, जिस युग में धर्म अपनी आत्मा खो चुका था और जातियों की दीवारें इंसानियत को बांध रही थीं। आज जब हम कबीर की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हैं, तो यह केवल श्रद्धांजलि का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का क्षण भी है।
समाज सुधारक कबीर: जात-पात के विरुद्ध एक क्रांति
कबीर ने समाज को जातिवाद और ऊँच-नीच की कुप्रथाओं से बाहर निकालने का कार्य किया। उन्होंने खुलकर कहा:
"जाती न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।।"
यह दोहा केवल काव्य नहीं, उस काल के सामाजिक ढांचे पर एक करारी चोट है। कबीर ने न केवल वर्ण व्यवस्था को प्रश्नांकित किया बल्कि शूद्रों, दलितों और स्त्रियों के मानवीय अधिकारों की वकालत की।
भक्ति आंदोलक: निर्गुण भक्ति का आलोक
कबीर भक्ति आंदोलन के उन संतों में से थे जिन्होंने ‘निर्गुण ब्रह्म’ की धारणा को प्रचारित किया। उनके लिए ईश्वर कोई मूर्ति नहीं था, वह एक चेतना था – साकार नहीं, निराकार:
"मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलास में।।"
यह भाव कबीर को रामानंद जैसे संतों से जोड़ता है, लेकिन वे परंपरा से अलग खड़े होते हैं क्योंकि उनकी भक्ति में तर्क है, अनुभव है और जनपक्षधरता है।
धार्मिक समरसता: न हिन्दू, न मुसलमान
कबीर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी धर्म निरपेक्ष दृष्टि थी। एक ओर वे हिंदू कर्मकांडों पर प्रहार करते हैं तो दूसरी ओर मुसलमानों की रीति-रिवाजों की आलोचना करने से भी नहीं चूकते:
"हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना।
आपस में दोउ लरै मरै, मरम न जाने कोय।।"
कबीर का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि धर्म का सार कर्म और आचरण में है, न कि बाहरी प्रतीकों में। आज के सांप्रदायिक संघर्षों से त्रस्त समाज को कबीर की यही दृष्टि संजीवनी प्रदान कर सकती है।
भाषा और जनता से जुड़ाव: सहज बोली में गूढ़ बात
कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी – एक मिश्रित भाषा जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और अरबी-फारसी के शब्दों का सहज उपयोग है। वे संस्कृत के ठाट में नहीं, लोकभाषा के लहजे में बात करते हैं – यही उन्हें जनता का कवि बनाता है।
उनके दोहे किसानों, मजदूरों, दस्तकारों की ज़िंदगी से निकले हैं। उन्होंने जुलाहे के रूप में अपना जीवन जीकर श्रम और सृजन को आध्यात्मिक अर्थ दिए।
कबीर की प्रासंगिकता: आज के भारत के लिए सबक
आज जब जाति-धर्म के नाम पर समाज को बाँटा जा रहा है, जब बाह्याचार को धर्म का पर्याय बना दिया गया है, और जब धार्मिक पहचान हिंसा का औजार बनती जा रही है – ऐसे समय में कबीर की वाणी एक तीखी चेतावनी की तरह सुनाई देती है।
कबीर हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वह है जो भीतर से उपजे, जो प्रेम और करुणा पर आधारित हो, जो अन्याय के विरुद्ध बोले और जो सबको जोड़ने का कार्य करे, न तोड़ने का।
कबीर केवल इतिहास नहीं, भविष्य की राह भी हैं
कबीर कोई बीते हुए युग के संत नहीं हैं। वे हर उस समय के लिए ज़रूरी हैं जब समाज आत्ममंथन से डरता है, जब धर्म सत्ता का उपकरण बनता है और जब मनुष्यता की आवाज़ को कुचला जाता है। कबीर की वाणी एक चेतावनी है, एक संवाद है और एक समाधान भी।
"कबीरा खड़ा बाज़ार में, लिए लुकाठी हाथ।
जो घर फूँके आपना, चले हमारे साथ।।"
यह निमंत्रण आज भी वैसा ही है – खुद को जलाकर समाज को रोशन करने का साहस रखने वालों के लिए।
कबीर का स्मरण केवल भक्ति के गीत गाने का अवसर नहीं, बल्कि उनकी वाणी को आत्मसात करने का अवसर होना चाहिए। आज जब हमारा समाज अनेक प्रकार की विभाजक रेखाओं से गुजर रहा है, तब कबीर की निर्भीकता, उनकी मानवीयता और उनकी गहराई हमें नई राह दिखा सकती है।
What's Your Reaction?