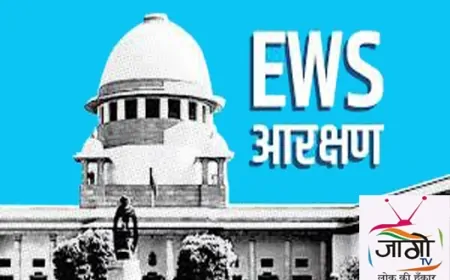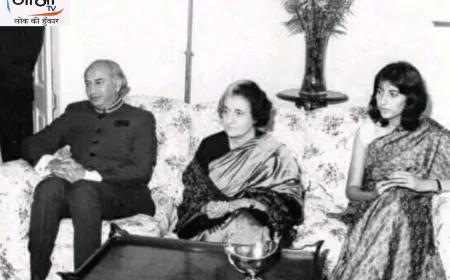प्रेमचंद की साहित्यिक दृष्टि और सामाजिक चेतना: गाँव, किसान, दलित, स्त्री, मजदूर और पत्रकारिता के विमर्शों में प्रेमचंद की प्रासंगिकता
यह संपादकीय लेख हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक लेखक मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक दृष्टि और सामाजिक चेतना का विश्लेषण करता है। लेख में प्रेमचंद की रचनाओं के माध्यम से गाँव, किसान, दलित, स्त्री और मजदूर वर्ग के यथार्थपूर्ण चित्रण, भाषा की सहजता, पत्रकारिता में भूमिका, और उनकी आज की सामाजिक-राजनीतिक प्रासंगिकता पर गहन विमर्श किया गया है। प्रेमचंद को आज के भारत में पुनः पढ़ना, समझना और जीना क्यों जरूरी है, यह लेख इसी प्रश्न का उत्तर है।

प्रेमचंद: समाज के यथार्थ के लेखक - गाँव, दलित, स्त्री और श्रमिक चेतना की आवाज़
"साहित्य का काम केवल मनोरंजन नहीं, समाज का मार्गदर्शन करना है।" - प्रेमचंद
प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं थे, वे सामाजिक यथार्थ के सजग प्रहरी और भारतीय जनमानस के अंतरदृष्टा थे। उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण करना मात्र एक रस्म नहीं, बल्कि उनकी लेखनी की उस अग्नि को पुनः महसूस करना है, जो आज भी अन्याय, विषमता और अंधकार के विरुद्ध जल रही है।
प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएँ: यथार्थवाद, करुणा और नैतिक संघर्ष
प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने साहित्य को काल्पनिक जंजाल से निकालकर सामाजिक यथार्थ की जमीन पर खड़ा किया। उनके पात्र, घटनाएँ और कथानक हमारे आस-पास के जीवन से सीधे जुड़ते हैं। वे समाज के उस तबके को आवाज़ देते हैं जो सदियों से मौन था- किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, और हाशिए पर खड़ा आमजन।
उनकी कहानियों में यथार्थ का ताप, मानवीय करुणा की गहराई, और नैतिक द्वंद्व की तीव्रता है। 'गोदान' में होरी का जीवन-संघर्ष केवल एक किसान की कथा नहीं, भारतीय ग्रामीण जीवन की सामूहिक त्रासदी है। 'कफ़न' में अभाव के चलते संवेदना तक कुंद हो जाती है, यह चित्रण प्रेमचंद की यथार्थवादी शैली को अमर बनाता है।
उनकी भाषा सरल, संवादात्मक और लोकजीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने साहित्य को आभिजात्य से निकालकर जनसामान्य की थाली में परोसा।
गाँव और किसान जीवन का चित्रण: भूख, संघर्ष और सामाजिक अन्याय
प्रेमचंद ने सबसे पहले गाँव और किसान को साहित्य का केंद्रीय पात्र बनाया। वे मानते थे कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, और इस आत्मा को यदि कोई साहित्यकार समझ सका, तो वह प्रेमचंद थे।
'गोदान' में होरी के जीवन के माध्यम से उन्होंने किसानों की ज़मींदारी शोषण, कर्ज़, सामाजिक अपमान और धार्मिक ढोंग के बीच कैसे पिसते हैं, यह दिखाया। 'पूस की रात' में हल्कू का ठंड से बचने के लिए अलाव की बजाय नींद चुनना उस गरीबी की हद को दिखाता है जहाँ आवश्यकता नैतिकता से बड़ी हो जाती है।
गाँव उनके लिए केवल प्रकृति का सौंदर्य नहीं, एक राजनीतिक-सामाजिक युद्धभूमि था, जहाँ किसान, पशु, स्त्री, ठाकुर और पुजारी सभी एक जटिल व्यवस्था का हिस्सा हैं।
दलित और वंचित वर्ग का सशक्तिकरण: ‘सद्गति’ से ‘ठाकुर का कुआँ’ तक
प्रेमचंद पहले बड़े लेखक थे जिन्होंने दलित विषयों को गंभीरता से अपनी कहानियों में स्थान दिया। 'सद्गति' में दुखी चमार की मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं, सामाजिक ढांचे की क्रूरता का प्रतीक है। वह ब्राह्मण के लिए लकड़ी काटता है, पर उसकी लाश को छूने से भी इंकार किया जाता है।
'ठाकुर का कुआँ' में दलित स्त्री पानी भरने के लिए ठाकुरों के कुएँ से पानी लेना चाहती है, यह क्रिया उस समय क्रांति थी। प्रेमचंद ने यहाँ दलित प्रश्न को करुणा नहीं, अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया।
उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद और वर्गगत अन्याय के विरुद्ध लेखनी चलाई, हालांकि उनके दृष्टिकोण सुधारवादी थे, फिर भी यह उस युग में बहुत बड़ा कदम था।
स्त्री विमर्श: सहनशीलता से प्रतिरोध तक का साहित्यिक सफर
प्रेमचंद की स्त्रियाँ केवल पीड़िता नहीं हैं, वे प्रश्न करती हैं, संघर्ष करती हैं और सामाजिक बंधनों को तोड़ने का साहस भी रखती हैं।
'सेवासदन' में सुधा का वेश्यालय में जाना, फिर लौटकर समाजसेवी बनना स्त्री की स्वायत्तता को दर्शाता है। 'निर्मला' में विधवा की त्रासदी के माध्यम से उन्होंने दहेज, बाल विवाह और पितृसत्ता पर गहरी चोट की।
'प्रेमाश्रम', 'बड़े घर की बेटी' जैसी रचनाएँ भी स्त्री के आत्मसम्मान, विवेक और सामाजिक स्थिति को विवेचित करती हैं। प्रेमचंद के स्त्री पात्रों में आज की नारी की छवि भी दिखाई देती है, सोचने वाली, जूझने वाली और निर्णय लेने वाली।
मजदूर और श्रमिक विमर्श: वर्ग चेतना का आरंभ
प्रेमचंद ने अपने समय में ही मजदूर और श्रमिक वर्ग की पीड़ा को स्वर दिया। 'ईंधन' में लकड़ी ढोने वाली स्त्री, 'माँ' में श्रमजीवी स्त्री का बलिदान, 'बेटों वाली विधवा' में अकेली स्त्री की संघर्षगाथा, ये सब कहानियाँ वर्ग संघर्ष के बीज बोती हैं।
उन्होंने मजदूरों को केवल आर्थिक समस्या नहीं, मानव गरिमा का विषय बनाया। यह वही श्रमिक हैं जो आज भी कारखानों, खेतों और ईंट-भट्टों में काम करते हुए अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं।
प्रेमचंद की भाषा नीति: जनभाषा की प्रतिष्ठा
प्रेमचंद ने साहित्य की भाषा को दरबार और मंदिर से निकालकर खेत-खलिहान और चौपाल तक पहुँचाया। उन्होंने खड़ी बोली, उर्दू और हिंदी के सहज मिश्रण से ऐसी भाषा गढ़ी जो आमजन की थी।
उनकी भाषा में न तो कृत्रिमता है, न दुरूहता। यह भाषा संवाद करती है, टकराती है, और धीरे-धीरे पाठक के भीतर उतर जाती है। आज जब हिंदी साहित्य elitism और कठिनता की ओर बढ़ रहा है, प्रेमचंद की भाषा प्रेरणा देती है कि साधारण में ही असाधारण है।
पत्रकार प्रेमचंद: विचारों की निर्भीकता
प्रेमचंद केवल कथाकार नहीं, एक गंभीर पत्रकार भी थे। ‘ज़माना’, ‘हंस’ और ‘माधुरी’ जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने लेखनी को जनता की आवाज़ बनाया।
उनकी पत्रकारिता में ब्रिटिश सत्ता की आलोचना, जाति-पंथ पर सवाल, और साहित्य की भूमिका पर विवेचना मिलती है। वे पत्रकारिता को वैचारिक ईमानदारी का माध्यम मानते थे, न कि सूचना के व्यापार का। आज जब पत्रकारिता कॉर्पोरेट और राजनीतिक दबाव में है, प्रेमचंद की निर्भीक पत्रकारिता हमें दिशा देती है।
प्रेमचंद की समकालीन प्रासंगिकता: आज फिर उन्हें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है?
आज भारत में किसानों की आत्महत्या, दलितों पर अत्याचार, स्त्रियों पर हिंसा, मजदूरों का पलायन, और पत्रकारों की हत्या, ये सब प्रेमचंद की रचनाओं को फिर से पढ़ने की माँग करते हैं।
'गोदान' में जो अन्याय है, वह आज भी बदला नहीं है। 'सद्गति' की जातिवादी सच्चाई गाँव-शहर दोनों में विद्यमान है। 'सेवासदन' की स्त्री आज भी ट्रोलिंग और यौन हिंसा की शिकार है।
प्रेमचंद की रचनाएँ आज भी केवल साहित्यिक पूंजी नहीं, नागरिक चेतना का उपकरण हैं।
विचारधारा और वैचारिक उत्तराधिकार: प्रेमचंद की विरासत
प्रेमचंद की विचारधारा गांधीवादी करुणा, लोहियावादी सामाजिक न्याय, और मार्क्सवादी वर्ग-संघर्ष के बीच संतुलन रखती है। वे जनवादी लेखक थे, जिन्होंने आदर्श और यथार्थ के बीच संवाद की भाषा बनाई।
उनकी वैचारिक परंपरा फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म साहनी, नागार्जुन, अमृतलाल नागर और भी आगे के कथाकारों में जीवित रही। वे हमारे साहित्य के 'संविधान निर्माता' की भूमिका में हैं, जिनकी मानवीय दृष्टि कालातीत है।
प्रेमचंद होना आज भी जरूरी है
आज जब साहित्य बाजार का उत्पाद बन गया है, जब लेखक पुरस्कारों के लिए लिखते हैं और पत्रकारिता सत्ता की गोद में बैठी है, प्रेमचंद को पढ़ना और समझना एक सांस्कृतिक प्रतिरोध है।
प्रेमचंद को याद करना उनकी रचनाओं को दोहराना नहीं, उनके विचारों को जीना है। वे आज भी हमारे भीतर एक सवाल की तरह जीवित हैं, "क्या साहित्य समाज को बदल सकता है?"
और इसका उत्तर है- हाँ, अगर वह प्रेमचंद जैसा हो।
प्रेमचंद को नमन, कलम के उस सच्चे सिपाही को जिसने अपने शब्दों से समाज की सबसे गहरी चोटों पर मरहम भी रखा और चेतावनी भी दी।
What's Your Reaction?