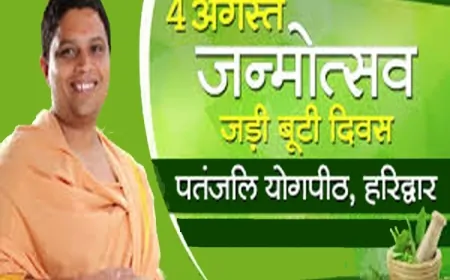लोकतांत्रिक राज्य में शक्तियों का पृथक्करण : संविधान की सुरक्षा व लोकतंत्र की मजबूती
यह लेख शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें लोकतंत्र की स्थायिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व बताया गया है। आलेख में फेडरलिस्ट पेपर्स, भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र को तानाशाही प्रवृत्तियों से बचाता है, शासन में संतुलन तथा जवाबदेही लाता है और गणतंत्र को सशक्त रखता है।

लोकतांत्रिक राज्य में शक्तियों का पृथक्करण : लोकतंत्र की नींव
लोकतंत्र की शक्ति केवल मताधिकार या चुनावी प्रक्रिया में नहीं, बल्कि उसकी संस्थाओं की बनावट और संचालन में छुपी होती है। शक्तियों का पृथक्करण उस राज्य व्यवस्था का मूलाधार है, जिससे 'सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की' बनी रह सके। यदि ये विभाजन धुंधला या कमजोर पड़ जाए, तो लोकतंत्र जल्दी ही सत्ताकेंद्रित और तानाशाही प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हो सकता है।
लोकतांत्रिक राज्य में शक्तियों की अवधारणा
लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, न्याय, और समानता की अवधारणा है। किंतु उसकी मजबूती उन्हीं संस्थागत व्यवस्थाओं में निहित है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) लोकतंत्र का मूल तत्व है, जो उसे तानाशाही से बचाता है और उसे न्यायसंगत एवं उत्तरदायी बनाता है।
शक्तियों का पृथक्करण: अवधारणा और आवश्यकताएँ
शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत सरकार के तीन प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र एवं अधिकारों की स्पष्ट सीमाएँ तय करने की बात करता है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी अंग पूर्ण अधिकार न प्राप्त कर सके, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। अमेरिकी संविधान के निर्माण के समय James Madison ने Federalist No.47 में लिखा था: "जब विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या समूह में केंद्रित हो जाती हैं, तब स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। अगर न्यायपालिका भी उसमें मिल जाए तो स्वेच्छाचार की उत्पत्ति निश्चित है।"
शक्तियों के पृथक्करण का ऐतिहासिक विकास
Montesquieu (फ्रांसीसी विचारक) ने अपने ग्रंथ 'स्पिरिट ऑफ लॉज' (1748) में पहली बार संस्थागत रूप से शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को रखा। उन्होंने कहा कि "सत्ता के तीन अंगों का पृथक रहना आवश्यक है; तभी नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है।"
यही विचार अमेरिकी संविधान में प्रतिध्वनित हुए। James Madison ने Federalist No.47 में स्पष्ट किया कि सत्ता का केंद्रीकरण स्वतंत्रता का विनाश करता है। भारत के संविधान निर्माता भी इसी सिद्धांत से प्रभावित हुए।
शक्तियों का पृथक्करण: तीन अंग, विशिष्ट जिम्मेदारियाँ
1. विधायिका (Legislature)
o कानून बनाना, बजट पारित करना और सरकार की जवाबदेही तय करना।
o उदाहरण: संसद में किसी नए कानून का मसौदा तैयार और पारित किया जाता है।
2. कार्यपालिका (Executive)
o संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन, प्रशासन संचालन।
o उदाहरण: प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री प्रशासनिक निर्णय लेते हैं, विभिन्न मंत्रालय नीतियाँ लागू करते हैं।
3. न्यायपालिका (Judiciary)
o कानून की व्याख्या, नागरिक अधिकारों की रक्षा, कार्यपालिका और विधायिका की जांच।
o उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नागरिकों द्वारा सरकार के निर्णय को चुनौती दी जाती है; NJAC केस में नियुक्ति की प्रक्रिया पर न्यायिक समीक्षा हुई।
लोकतंत्र को मजबूती कैसे मिलती है?
भारत सहित दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में शक्तियों का पृथक्करण सीधे-सीधे लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा है:
· सत्ता का दुरुपयोग रोकना: शासकों या सरकार द्वारा अधिकारों के केंद्रीकरण से उत्पन्न भ्रष्टाचार, तानाशाही प्रवृत्ति और मनमानी को विभाजित सत्ता प्रणाली ही नियंत्रित कर सकती है।
· न्याय की स्वतंत्रता: Federalist No.78 के अनुसार, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने चाहिए, ताकि वह अन्य अंगों के विवेकाधीन कार्यों की समीक्षा कर सके और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित कर सके।
· संवैधानिक संतुलन: Federalist No.51 में बार-बार जोर दिया गया है कि सरकार के अंगों के बीच संतुलन और परस्पर चेक्स एवं बैलेंस न हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ दिखावा रह जाती है।
· सत्ता का विकेंद्रीकरण: सत्ता के विभाजन से शासन का लोकतांत्रिक होना और नागरिकों के प्रति उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
उदाहरण : भारत में शक्तियों के पृथक्करण का प्रभाव
1. IR Coelho v. State of TN (2007): सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे (basic structure) को संसद नहीं बदल सकती। Federalist Nos.47, 48 और 51 पर आधारित यह सिद्धांत कानून बनाने की संसद की शक्ति और न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति के बीच संतुलन निर्मित करता है।
2. Manoj Narula v. Union of India (2014): न्यायपालिका ने राजनीतिक नैतिकता और संसद के अधिकारों की सीमाएँ तय कीं संविधान की सर्वोच्चता और checks and balances की जरूरत पर बल दिया गया।
3. NJAC केस: न्यायाधीश नियुक्ति अधिनियम को चुनौती देते हुए कोर्ट ने कहा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की आत्मा है। यदि सरकार स्वयं न्यायाधीश नियुक्त करेगी तो न्याय का निष्पक्ष वितरण असंभव हो जाएगा।
4. राज्यपाल का दुरुपयोग: मणिपुर, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सरकार गठन के समय राज्यपाल द्वारा असंवैधानिक तरीके से बहुमत की अनदेखी, कार्यपालिका के अतिक्रमण का उदाहरण है, जिसके विरुद्ध न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया।
शक्तियों के पृथक्करण के विघटन के परिणाम
अगर संसद, सरकार और न्यायपालिका की सीमाएँ धुंधली हो जाएँ-
· संसद सरकार के इशारे पर मनमाने कानून बनाने लगे,
· सरकार न्यायपालिका को प्रभावित करे,
· न्यायपालिका निज लाभ या दबाव में निर्णय दे, तो लोकतंत्र का आधार हिल जाता है: नागरिक अधिकारों का हनन, असहमति की आवाज दबाना, तानाशाही का प्रवेश ये सब देखने को मिल सकता है।
अंतरराष्ट्रीय उदाहरण
· अमेरिका:
Watergate Scandal में अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों के दुरुपयोग को न्यायपालिका ने पूरी तरह रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राष्ट्रपति Nixon को इस्तीफा देना पड़ा।
· पाकिस्तान:
यहाँ शक्तियों की सीमाएँ बार-बार टूटती रहीं, सेना (कार्यपालिका) ने अक्सर सरकार (विधायिका) का तख्ता पलट दिया, न्यायपालिका भी दबाव में रही नतीजा, स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बन पाई।
आधुनिक चुनौतियाँ
· लोकप्रियता के आधार पर निर्णय:
कोई सरकार अगर लोक लोकप्रियता या बहुसंख्यकवाद का लाभ उठाकर विधायिका या प्रशासन को नियंत्रित करने लगे, तो शक्तियों का पृथक्करण संकट में आ जाता है।
· जज की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप:
NJAC मामला इसका उदाहरण है, जिसमें न्यायाधीश नियुक्त करने के अधिकार को सरकार खत्म करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित की।
भारतीय प्रसंग
भारतीय संविधान ने वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाते हुए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग पहचान दी है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर विभिन्न मामलों में फेडरलिस्ट पेपर्स का हवाला देते हुए शक्तियों के व्यक्तिगत व स्वतंत्र होने की आवश्यकता रेखांकित की है, जैसे कि IR Coelho v. State of TN (2007), Madras Bar Association v. Union of India (2022), Manoj Narula v. Union of India (2014) आदि में। इन फैसलों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक सरकार के अंग स्वतंत्र व संतुलित रहेंगे, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा।
आज के संदर्भ में महत्व
आज, जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों एवं जिम्मेदारियों को लेकर तनाव या संघर्ष पैदा होता है, तब इन सबसे ऊपर संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका निर्णायक हो जाती है। अगर शक्तियों का पृथक्करण टूटता है, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर पड़ती हैं, अधिकारों का हनन होता है, जवाबदेही खत्म होती है, और नागरिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है।
लोकतंत्र की स्थायिता और पृथक्करण
लोकतांत्रिक राज्य के स्थापत्य में शक्तियों का पृथक्करण एक अनिवार्य बुनियाद है। इससे ही सत्ता में संतुलन रहता है, नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, और लोकतंत्र मजबूत होता है। इस सिद्धांत में कोई भी क्षणिक विचलन दीर्घकालिक नुकसान और विघटन का कारण बन सकता है। लोकतन्त्र सिर्फ चुनाव नहीं, मजबूत संस्थाएँ, जवाबदेही और कानून का राज है। यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र, निर्भीक और एक दूसरे की शक्ति सीमित करने वाले रहें, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है, और देश में नागरिक स्वतंत्रता टिकती है। आज भी फेडरलिस्ट पेपर्स के सूत्रों, भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के मिसालों द्वारा यह सिद्धांत प्रासंगिक है, शक्तियों का पृथक्करण ही लोकतंत्र की असली नींव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण केवल सैद्धांतिक आवश्यकता नहीं, अपितु व्यवहारिक लोकतंत्र की आत्मा है।
What's Your Reaction?