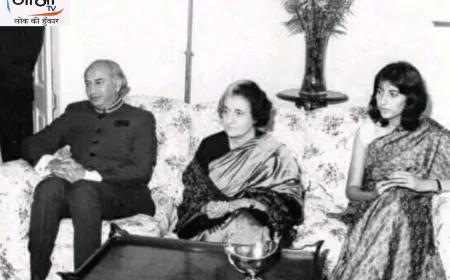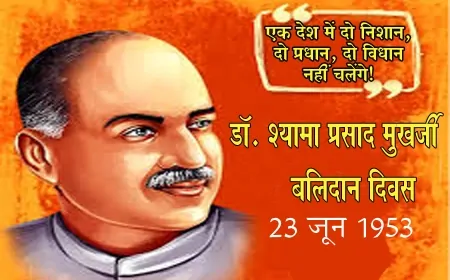हिंदी दिवस 2025: भाषा, पहचान और नीतिगत विमर्श का शैक्षणिक मूल्यांकन
हिंदी दिवस (14 सितंबर) पर यह शोधपरक लेख संविधान सभा की बहसों, जनगणना आँकड़ों, डिजिटल इंडिया रिपोर्ट और नई शिक्षा नीति (2020) के संदर्भ में हिंदी की स्थिति, चुनौतियों और वैश्विक संभावनाओं का अकादमिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
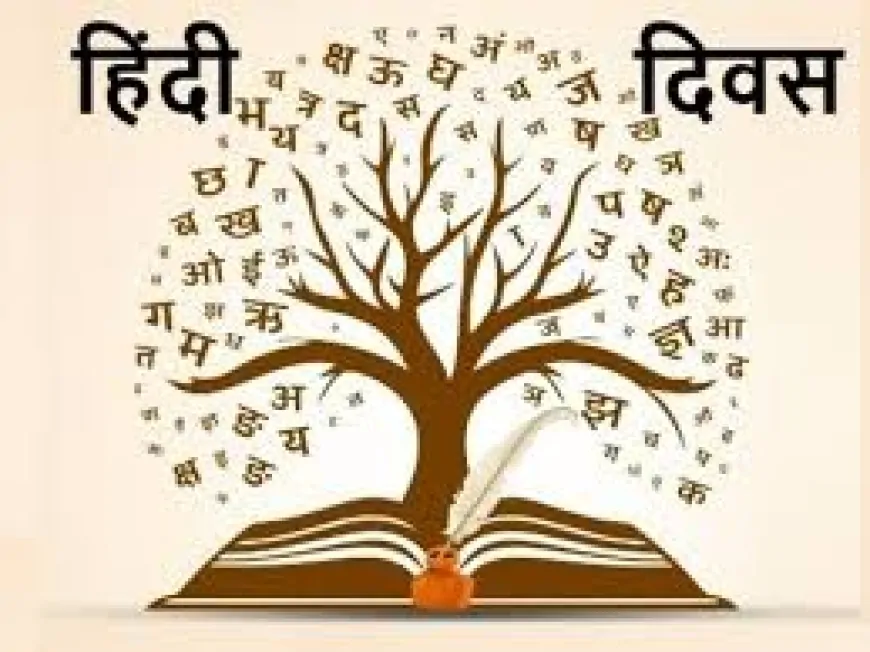
हिंदी दिवस: भाषा, पहचान और नीति का अकादमिक परिप्रेक्ष्य
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संविधान सभा और राजभाषा का प्रश्न
14 सितंबर 1949 का दिन भारतीय संविधान और भाषा-राजनीति के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय किसी भावनात्मक आग्रह का परिणाम नहीं था, बल्कि गहन बहस और सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ का प्रतिफल था। संविधान सभा की कार्यवाहियों (संविधान सभा वाद-विवाद, खंड 9, 10 और 11) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भाषा-प्रश्न पर तीव्र मतभेद थे।
महावीर त्यागी, पुरुषोत्तमदास टंडन और पं. गोविंद बल्लभ पंत जैसे सदस्यों ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम मानते हुए इसे राजभाषा बनाने की पैरवी की। दूसरी ओर, टी.टी. कृष्णमाचारी, गोपालस्वामी आयंगर और दक्षिण भारत के प्रतिनिधियों ने अंग्रेज़ी की निरंतरता और क्षेत्रीय भाषाओं की गरिमा पर बल दिया। अंततः एक समझौता सूत्र सामने आया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, किंतु अंग्रेज़ी को सहायक राजभाषा के रूप में 15 वर्षों तक (1965 तक) बनाए रखने का प्रावधान रखा गया।
भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भी यह निर्णय तर्कसंगत था। 1941 की जनगणना (जिसे 1951 की पहली स्वतंत्र भारत की जनगणना ने आगे पुष्ट किया) दर्शाती है कि हिंदी-भाषी जनसंख्या लगभग 40% थी। हिंदी का भौगोलिक विस्तार गंगा-यमुना के मैदान से लेकर मध्य भारत तक था, और साहित्यिक परंपरा तुलसीदास से प्रेमचंद तक पहले से ही राष्ट्रीय विमर्श की भाषा गढ़ चुकी थी।
इस प्रकार, हिंदी को राजभाषा घोषित करना एक राजनीतिक-सांस्कृतिक समझौता और ऐतिहासिक आवश्यकता दोनों का परिणाम था।
वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या लगभग 52.8 करोड़ (43.63%) है। यदि भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, अवधी आदि हिंदी की उपभाषाओं को शामिल कर लिया जाए, तो यह संख्या 60 करोड़ से अधिक हो जाती है। हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में बोलने वाले व्यक्तियों को जोड़ने पर यह आँकड़ा 80 करोड़ से अधिक तक पहुँचता है (Census of India, 2011: Language Tables)।
शिक्षा में हिंदी का प्रसार उल्लेखनीय है। UGC के आँकड़े बताते हैं कि स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य देश के सबसे अधिक नामांकन वाले विषयों में शामिल है। NCERT और CBSE ने हिंदी को स्कूल स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में बनाए रखा है। सरकारी उपयोगिता की दृष्टि से हिंदी केंद्र सरकार की मंत्रालयों, संसद की कार्यवाही और केंद्रीय प्रशासन में प्रमुख भाषा है।
हाल के ‘Languages in India’ (2019, लोक फाउंडेशन) सर्वेक्षण ने दर्शाया कि डिजिटल शिक्षा सामग्री, ई-गवर्नेंस और ग्रामीण संचार में हिंदी की उपयोगिता सबसे अधिक है। इससे हिंदी एक जनसंचार और शैक्षणिक साधन दोनों के रूप में स्थापित हुई है।
चुनौतियों का विवेचन
(क) उच्च शिक्षा और न्यायपालिका में अंग्रेज़ी की प्रधानता
भारत की न्यायपालिका अब भी अंग्रेज़ी पर निर्भर है। लॉ कमीशन की 216वीं रिपोर्ट (2008) और हाल की बहसें दर्शाती हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही मुख्यतः अंग्रेज़ी में होती है। उच्च शिक्षा, विशेषकर विज्ञान, तकनीक और विधि शिक्षा में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता बनी हुई है। यह स्थिति हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के अकादमिक विकास में बाधक है।
(ख) क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संतुलन
दक्षिण भारत में हिंदी-विरोधी आंदोलनों (1965, 1986) का ऐतिहासिक संदर्भ हमें सावधान करता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के समाजशास्त्रीय अध्ययनों (Annamalai, 2004; Pattanayak, 1990) से स्पष्ट है कि भाषा केवल संचार का साधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। हिंदी का प्रसार यदि क्षेत्रीय भाषाओं के क्षरण के रूप में देखा जाएगा, तो विरोध स्वाभाविक होगा।
(ग) भाषाई-सांस्कृतिक पहचान
समाजभाषाविज्ञान (Sociolinguistics) के अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि भाषा व्यक्ति की सांस्कृतिक स्मृति और सामूहिक पहचान से गहराई से जुड़ी होती है (Fishman, 1972; Srivastava, 2005)। अतः हिंदी का विकास तभी संभव है जब वह अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सह-अस्तित्व और परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया को अपनाए।
वैश्वीकरण और डिजिटल परिप्रेक्ष्य
डिजिटल क्रांति ने हिंदी को नया आयाम दिया है। KPMG–Google रिपोर्ट (2017) बताती है कि भारत में 2021 तक 53 करोड़ भारतीय भाषाओं के इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जिनमें से लगभग 38% हिंदी उपभोक्ता थे। हिंदी कंटेंट की वृद्धि दर अंग्रेज़ी से दोगुनी तेज़ है।
NITI Aayog की Digital India आँकड़े (2022) दर्शाते हैं कि सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण में हिंदी प्रमुख भूमिका निभा रही है। OTT प्लेटफ़ॉर्म (Netflix, Amazon Prime, SonyLiv) पर हिंदी सामग्री का उपभोग सबसे अधिक है। ई-कॉमर्स कंपनियाँ (Flipkart, Amazon, Meesho) हिंदी-इंटरफ़ेस को अपनी व्यावसायिक रणनीति का केंद्र बना रही हैं।
इस प्रकार, हिंदी केवल साहित्य या प्रशासन की भाषा नहीं रही, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार की निर्णायक शक्ति बन चुकी है।
नीतिगत संदर्भ: नई शिक्षा नीति (2020)
नई शिक्षा नीति (NEP-2020) में मातृभाषा/भारतीय भाषा में शिक्षा पर बल दिया गया है। नीति कहती है कि कक्षा 5 तक और संभव हो तो 8 तक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इससे हिंदी शिक्षण को अवसर मिलेगा, विशेषकर हिंदी पट्टी के राज्यों में।
हालाँकि, चुनौतियाँ भी हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर पाठ्यपुस्तकों, अनुसंधान सामग्री और तकनीकी शब्दावली की कमी है। राजभाषा विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों की नीतियाँ तुलनात्मक रूप से असमान हैं। जैसे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में हिंदी प्रशासनिक स्तर पर मजबूत है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में हिंदी के स्थान पर स्थानीय भाषाएँ प्राथमिकता पाती हैं।
संस्कृति और राष्ट्रीय एकता में योगदान
भाषा केवल संचार नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का सूत्र है। सांस्कृतिक अध्ययन (Niranjana, 1990; Pollock, 2006) बताते हैं कि हिंदी ने राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान एक साझा सांस्कृतिक मंच प्रदान किया। हिंदी सिनेमा, हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य ने विविध प्रांतों को एक सामान्य संवाद-क्षेत्र दिया। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी ने दलित साहित्य, स्त्री लेखन और ग्रामीण आख्यानों के माध्यम से समाज के हाशिये पर स्थित समुदायों को स्वर दिया है। सांस्कृतिक एकता और लोकतांत्रिक संवाद में हिंदी की भूमिका निर्विवाद है।
समाधान और अनुशंसाएँ
1. अनुवाद अध्ययन का संस्थानीकरण – क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी साहित्य के परस्पर अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर ‘Translation Studies’ को अनिवार्य बनाना।
2. डिजिटल टूल्स का विकास – हिंदी के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले AI, मशीन अनुवाद और NLP (Natural Language Processing) टूल्स का विकास।
3. द्विभाषिक शिक्षा – अंग्रेज़ी और हिंदी को परस्पर पूरक मानते हुए द्विभाषिक शिक्षा मॉडल को अपनाना।
4. क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संवाद – हिंदी को थोपे जाने की बजाय क्षेत्रीय भाषाओं के साथ सहयोग और आदान-प्रदान की रणनीति।
5. नीति-समानता – राज्यों के राजभाषा विभागों को एक राष्ट्रीय ढांचे में लाना ताकि कार्यान्वयन में असमानता दूर हो।
हिंदी दिवस केवल एक स्मरण दिवस नहीं, बल्कि भाषा-नीति, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के पुनर्मूल्यांकन का अवसर है। हिंदी आज केवल संचार का साधन नहीं रही; यह भारतीय पहचान की वाहक और डिजिटल युग में वैश्विक स्तर पर उभरती शक्ति है। संविधान सभा में जिस आशा के साथ हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, वह आशा आज नए संदर्भों में साकार हो रही है। किंतु, इस यात्रा को संतुलित और समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सह-अस्तित्व में विकसित हो।
जैसा कि भाषाविज्ञानी जोशुआ फिशमैन ने कहा था - “A language survives not by dominance but by mutual acceptance.” हिंदी का भविष्य भी इसी सिद्धांत पर निर्भर है।
ठीक है। मैंने आपके लेख के लिए शोधपूर्ण और SEO अनुकूलन दृष्टिकोण से शीर्षक, सार, टैग्स, कीवर्ड्स और गूगल प्रीव्यू तैयार किए हैं।
What's Your Reaction?