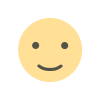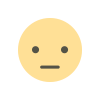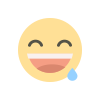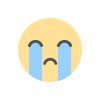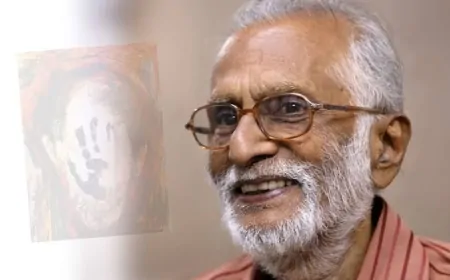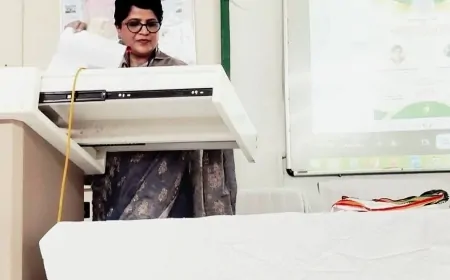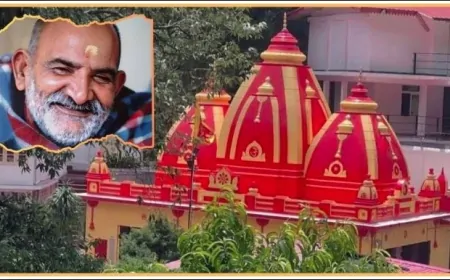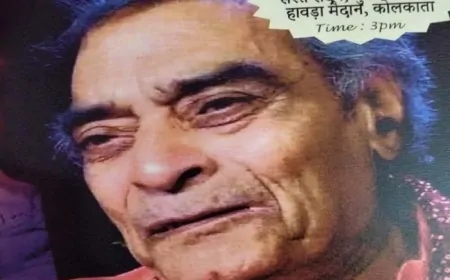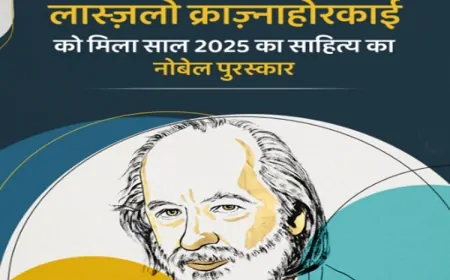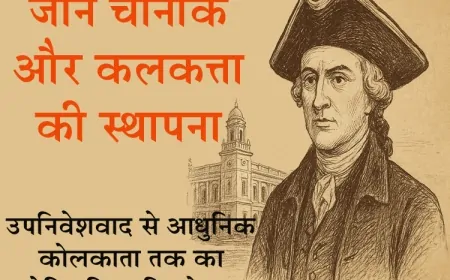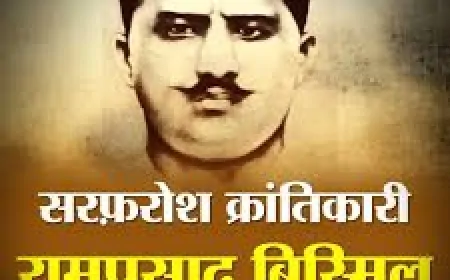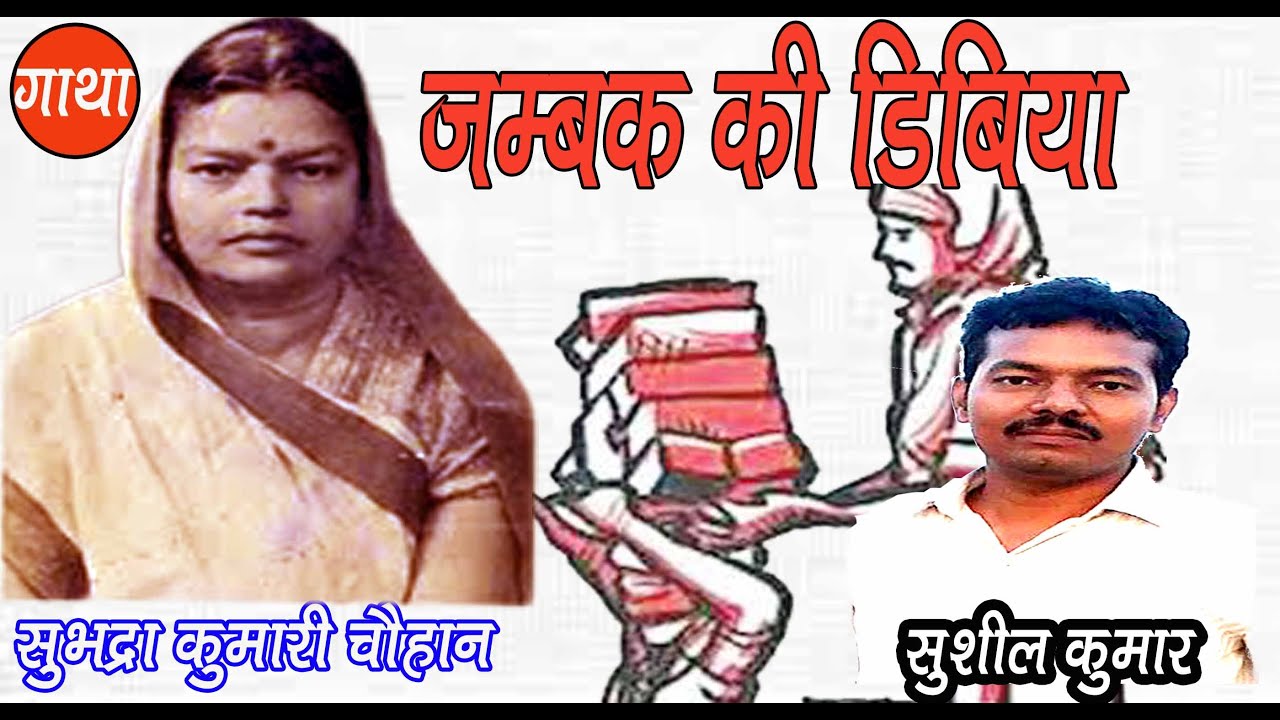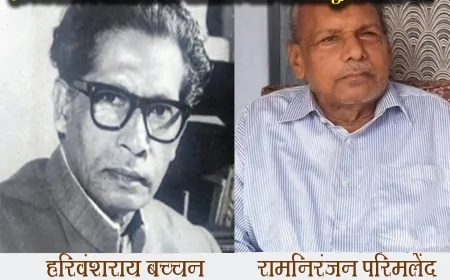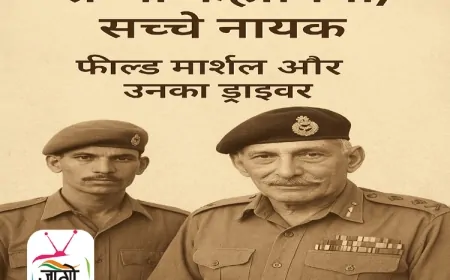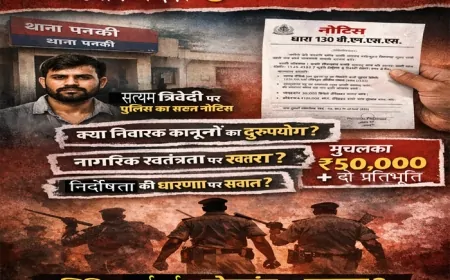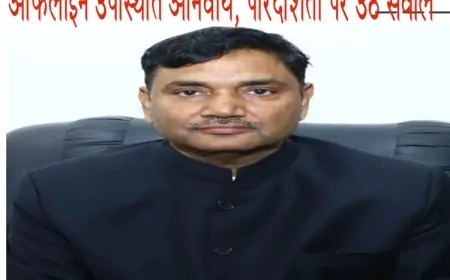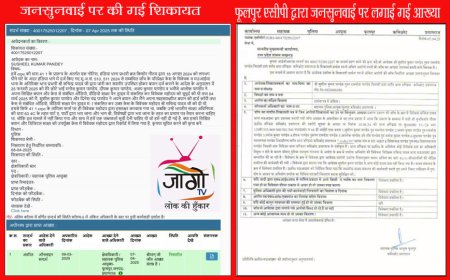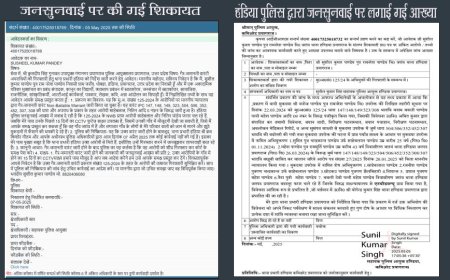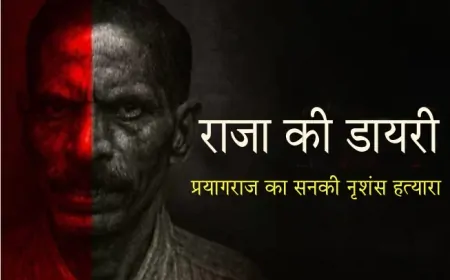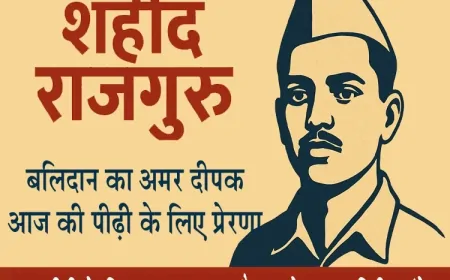लोक-लुभावन वादे या लोक-कल्याण? ‘फ्रीबीज’ पर भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट की ‘फ्रीबीज’ पर सख्त टिप्पणी के बाद कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी लोकलुभावनवाद पर गहन विश्लेषण। क्या मुफ्त योजनाएँ विकास में बाधा हैं?

एक टिप्पणी, अनेक प्रश्न
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘फ्रीबीज’ मुफ्त सुविधाओं की चुनावी घोषणाओं पर गंभीर टिप्पणी की। Tamil Nadu Electricity Distribution Corporation से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूछा कि जब अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में चल रहे हैं, तब वे मुफ्त भोजन, मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली और प्रत्यक्ष नकद अंतरण जैसी योजनाओं पर इतना व्यय कैसे कर रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी केवल न्यायिक अवलोकन नहीं, बल्कि लोकतंत्र के आर्थिक स्वास्थ्य पर उठाया गया मूल प्रश्न है। क्या हम विकास की कीमत पर लोकप्रियता खरीद रहे हैं?
‘फ्रीबीज’ और ‘कल्याणकारी योजनाएँ’: एक आवश्यक भेद
बहस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हर सरकारी सहायता को ‘फ्रीबीज’ कहना उचित नहीं। भारत का संविधान राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित करता है। नीति-निदेशक तत्व राज्य को यह दायित्व देते हैं कि वह सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे।
- मुफ्त राशन - खाद्य सुरक्षा
- छात्रवृत्ति या साइकिल योजना - शिक्षा में समान अवसर
- कृषि सब्सिडी - ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संरक्षण
- स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ - जीवन रक्षा
ये योजनाएँ सामाजिक न्याय के उपकरण हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सहायता का उद्देश्य सामाजिक सशक्तिकरण से हटकर चुनावी लाभ बन जाता है। जब ‘मुफ्त’ का वितरण आवश्यकता के बजाय राजनीतिक गणित से संचालित होता है, तब वह कल्याण नहीं, लोक-लुभावनवाद बन जाता है।
न्यायालय की चिंता: आर्थिक विवेक का प्रश्न
न्यायालय ने तीन मूल प्रश्न उठाए:
1. धन का स्रोत क्या है?
2. क्या विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन बच रहे हैं?
3. क्या चुनाव पूर्व घोषणाएँ लोकतांत्रिक निष्पक्षता को प्रभावित कर रही हैं?
यदि किसी राज्य का अधिकांश बजट वेतन, पेंशन और मुफ्त योजनाओं में व्यय हो जाए, तो पूंजीगत व्यय जैसे सड़कें, अस्पताल, उद्योग, अनुसंधान के लिए धन सीमित रह जाता है। राजकोषीय अनुशासन के लिए बनाए गए FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) ढाँचे का उद्देश्य यही है कि राज्य अनियंत्रित घाटे में न जाएँ। किंतु कई राज्य कर्ज लेकर योजनाएँ चला रहे हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ बढ़ रहा है।
टैक्सदाता और नैतिक अर्थशास्त्र
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा “यह पैसा कौन देगा?” उत्तर स्पष्ट है टैक्सदाता। जब करदाता यह देखता है कि उसका पैसा उत्पादक निवेश के बजाय अल्पकालिक लाभ बाँटने में खर्च हो रहा है, तो कर-नैतिकता कमजोर होती है। यह प्रश्न केवल आर्थिक नहीं, नैतिक भी है - क्या कर का उपयोग समान और न्यायपूर्ण है?
चुनावी राजनीति: घोषणाओं का मौसम
भारतीय राजनीति में चुनाव से ठीक पहले योजनाओं की घोषणा एक सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है। मुफ्त बिजली की सीमा बढ़ाना, महिलाओं को मासिक भत्ता, युवाओं को नकद प्रोत्साहन, मुफ्त गैजेट्स। ऐसी घोषणाएँ मतदाताओं को आकर्षित करती हैं, परंतु दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। न्यायालय का संकेत है कि राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्रों में वित्तीय स्रोत स्पष्ट करने चाहिए।
क्या बिना सहायता संभव है विकास?
यह भी उतना ही सत्य है कि भारत में गरीबी और असमानता अभी भी व्यापक है।
- करोड़ों परिवारों की आय अस्थिर है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित हैं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजी व्यय भारी है।
ऐसी स्थिति में राज्य यदि सहायता न दे, तो सामाजिक असंतुलन और बढ़ सकता है। इसलिए बहस ‘मुफ्त बनाम नहीं’ की नहीं, बल्कि ‘कैसे और किसे’ की है।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
विश्व के कई विकसित देशों में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ है- बेरोजगारी भत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा अनुदान, परंतु वहाँ इन योजनाओं के लिए कर संरचना मजबूत है और राजकोषीय अनुशासन कड़ा है। भारत में चुनौती यह है कि सीमित राजस्व के साथ व्यापक सामाजिक अपेक्षाएँ जुड़ी हैं।
संभावित समाधान: संतुलन की दिशा
1. लक्षित वितरण: केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ।
2. समय-सीमा: स्थायी मुफ्त योजनाओं के बजाय सीमित अवधि की सहायता।
3. पारदर्शिता: हर योजना का लागत-लाभ विश्लेषण सार्वजनिक हो।
4. रोजगार-आधारित मॉडल: प्रत्यक्ष नकद की बजाय कौशल विकास और रोजगार सृजन।
5. स्वतंत्र मूल्यांकन: चुनाव आयोग या वित्त आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा घोषणाओं की वित्तीय समीक्षा।
लोकतंत्र की परिपक्वता: मतदाता की भूमिका
लोकतंत्र केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं; मतदाता की भी है। यदि मतदाता तात्कालिक लाभ के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो राजनीतिक दल उसी दिशा में नीतियाँ बनाएँगे। परिपक्व लोकतंत्र में मतदाता यह पूछते हैं
- क्या यह योजना टिकाऊ है?
- क्या इससे रोजगार बढ़ेगा?
- क्या इससे दीर्घकालिक विकास होगा?
न्यायपालिका की भूमिका: चेतावनी, हस्तक्षेप नहीं
कुछ आलोचक कह सकते हैं कि न्यायालय नीति-निर्माण में दखल दे रहा है। परंतु, न्यायालय की भूमिका यहाँ केवल चेतावनी देने की है राजकोषीय अनुशासन और संवैधानिक संतुलन की याद दिलाने की। यह लोकतंत्र में संस्थागत संवाद का हिस्सा है।
विवेकपूर्ण कल्याण की ओर
भारत को न तो अंध-लोकलुभावनवाद चाहिए, न ही कठोर आर्थिक संकीर्णता। हमें चाहिए संतुलित, लक्षित और टिकाऊ कल्याणकारी नीतियाँ। यदि राज्य रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग पर निवेश बढ़ाए, तो नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। तब मुफ्त वितरण की आवश्यकता स्वतः घटेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक अवसर है राजनीति, अर्थशास्त्र और लोकतंत्र के बीच संतुलन साधने का अवसर।
अंततः प्रश्न यही है: क्या हम अल्पकालिक लाभ की राजनीति को चुनेंगे या दीर्घकालिक विकास की नीति को? भारत का भविष्य इसी उत्तर पर निर्भर करता है।
What's Your Reaction?