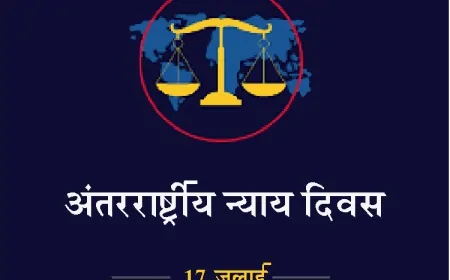जात-पांत बनाम जन-जागरण: क्या बिहार फिर पूछेगा – 'मैं कौन हूँ?'
यह संपादकीय बिहार के इतिहास में सामाजिक परिवर्तन के पुरोधाओं – जैसे डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, नागार्जुन, रेणु आदि के संघर्षों और सपनों की पड़ताल करता है। यह विश्लेषण करता है कि कैसे इन विभूतियों की वैचारिक चेतना के बावजूद, आज बिहार जातिवादी ध्रुवीकरण में उलझा हुआ है। लेख इस ऐतिहासिक प्रश्न को पुनः उठाता है - ‘मैं कौन हूं?’ और बिहार से ही एक नई संपूर्ण क्रांति की जरूरत को रेखांकित करता है, जो इस बार जात-पात की सीमाओं को तोड़कर आए।

मैं कौन हूँ? – बिहार की आत्मचेतना और एक नई संपूर्ण क्रांति की पुकार
बिहार की धरती ने भारतीय राजनीति, समाज और साहित्य को ऐसे अनगिनत मोती दिए हैं, जिनकी चमक ने देश की दिशा बदल दी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद से लेकर जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, नागार्जुन, रेणु और दिनकर तक इन सभी विभूतियों ने जाति, वर्ग और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर समाज की बुनियादी संरचना को बदलने का सपना देखा था। यह धरती ‘संपूर्ण क्रांति’ की जननी रही है, जहाँ जनसंघर्षों ने सत्ता की नींव हिला दी, और एक नई चेतना का संचार किया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: जाति का नकार और समता का उद्घोष
गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी:
बिहार की भूमि पर जन्मी बौद्ध और जैन परंपराएँ जाति आधारित श्रेणीकरण को त्यागने का प्रथम वैचारिक प्रयास थीं।
बुद्ध ने कहा: 'न जातिना ब्राह्मणो होति' (जाति से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है)।
महावीर ने 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत से हिंसा और भेदभाव का खंडन किया।
रामानुजाचार्य का वैष्णव सुधारवाद:
11वीं सदी में बिहार की यात्रा के दौरान उन्होंने ‘भक्ति को जाति से ऊपर’ बताया। उनके अनुयायी कहते हैं, 'भगवान की भक्ति में ऊँच-नीच नहीं होती'। इन परंपराओं की जड़ें बिहार की मिट्टी में थीं, लेकिन आज वही समाज जातीय खांचों में बंटा हुआ है।
स्वतंत्रता संग्राम से सामाजिक चेतना तक: एक विचारधारा का क्षरण
डॉ. राजेंद्र प्रसाद:
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के पहले राष्ट्रपति। उन्होंने बार-बार कहा कि - 'जाति हमें बाँटती है, संविधान हमें जोड़ता है।'
जयप्रकाश नारायण (JP):
JP का आंदोलन जाति के विरुद्ध आत्मचेतना की पुकार था - 1974 में जब संपूर्ण क्रांति का उद्घोष हुआ, तो यह राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि मूल्य-आधारित सामाजिक क्रांति की माँग थी। परंतु संपूर्ण क्रांति के बाद जातिगत समीकरणों की राजनीति ने उसी चेतना को अवशोषित कर लिया।
समाजवाद की विचारधारा और उसका जातीय अपहरण
राममनोहर लोहिया:
उन्होंने कहा: 'पिछड़ों को साठ प्रतिशत दो' - यह सामाजिक न्याय के लिए था, न कि जातिगत वर्चस्व के लिए। परंतु राजनीतिक दलों ने इसे 'जाति आधारित आरक्षण' के बहाने सत्ता की सीढ़ी बना लिया।
कर्पूरी ठाकुर:
वे जाति विरोधी नेता थे, जिन्होंने 'कर्म आधारित समता' का सपना देखा। पर उनकी आरक्षण नीति को बाद में ‘यादव बनाम सवर्ण’ राजनीति में बदल दिया गया। लोहिया और कर्पूरी के विचारों का उपयोग कर जातिवादी राजनीति ने उन्हें ही विस्मृत कर दिया।
साहित्य में जाति-चेतना बनाम समता की पुकार
नागार्जुन (यात्री):
उन्होंने ‘भोजपुरियों’ और दलितों की आवाज़ को काव्य में उतारा:
'मैं किसान तोड़ता हल,
मैं हूँ जनता की आवाज़'
फणीश्वरनाथ रेणु:
'मैला आँचल' में उन्होंने दिखाया कि ग्राम्य समाज किस तरह जातीय जड़ता में फँसा है और उससे मुक्त होना चाहता है।
अज्ञेय (सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन):
उनका लेखन आत्मचिंतन पर आधारित था। उन्होंने ‘व्यक्ति बनाम समाज’ के द्वंद्व को उजागर किया, जिसमें जाति एक बाधा बनकर सामने आती है। साहित्य ने जाति पर तीखा प्रहार किया, पर राजनीति ने उसे चुनावी रणनीति बना दिया।
सामाजिक कार्यकर्ता: समरसता के योद्धा
सुधा वर्गीज: दलित और मुसहर महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने शहरी सीमा से बाहर जाकर कार्य किया। उनके NGO ने ‘जाति के पार जाकर गरिमा’ के लिए काम किया।
बिंदेश्वरी पाठक: सुलभ शौचालय आंदोलन के जरिए उन्होंने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा: 'सफाई कर्मियों की जाति नहीं होती, उनका कर्म ही पूजा है।' इन कार्यकर्ताओं ने जाति नहीं, इंसानियत को प्राथमिकता दी।
वर्तमान स्थिति: जाति का बाज़ारीकरण और राजनीतिक गठबंधन
बिहार की राजनीति में आज Caste Mapping, Social Engineering और Micro-Targeting जैसे शब्द प्रचलित हैं। जाति आधारित संगठनों (जैसे भूमिहार ब्राह्मण महासभा, कोयरी-यादव एकता मंच, कुशवाहा महासंघ) के इर्द-गिर्द राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बना रहे हैं। नितीश कुमार जैसे नेताओं ने समता पार्टी की शुरुआत 'जाति विरोधी' एजेंडा से की, लेकिन आज वही राजनीति जाति-गणित के कुशलतम प्रयोग में बदल गई है। यह सब जन प्रतिनिधित्व नहीं, जाति प्रतिनिधित्व बन चुका है।
शिक्षण, मीडिया और नवउदारवाद: जाति की पुनर्संरचना
शिक्षा का विघटन:
सरकारी विद्यालयों में मूल्य शिक्षा समाप्त है।
इतिहास को जाति आधारित श्रेणियों में पढ़ाया जा रहा है, 'यह राजा यादव था, वह ब्राह्मण था…'
मीडिया में जाति की ब्रांडिंग:
जातियों पर आधारित टीवी रिपोर्ट: 'यादव बहुल इलाका', 'सवर्णों की गोलबंदी', आदि।
YouTube और WhatsApp पर जातीय गौरव के नाम पर उग्रवादी भावनाएँ फैलाई जा रही हैं।
नवउदारवाद में जाति एक नया Market Segment बन गया
जातीय पहचान पर आधारित प्रॉडक्ट मार्केटिंग, सोशल कैम्पेनिंग और यहाँ तक कि JEE/UPSC कोचिंग संस्थानों में भी 'हमारी जाति का टॉपर' की घोषणाएँ।
समाधान: क्या एक नई ‘संपूर्ण क्रांति’ संभव है?
'जब हर नागरिक अपनी जाति से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को समझेगा, तभी असली संपूर्ण क्रांति होगी।'- डॉ. राम मनोहर लोहिया
पुनरुद्धार की रणनीति:
नव-साक्षरता आंदोलन: शिक्षा में जाति नहीं, संवैधानिक मूल्यों का समावेश।
साहित्यिक पुनर्जागरण: नई पीढ़ी को नागार्जुन, रेणु, दिनकर से जोड़ना।
सामाजिक उद्यमिता: जाति-रहित पंचायत मॉडल, युवाओं की गैर-जातीय लीडरशिप।
नैतिक राजनीति का निर्माण: नई पीढ़ी के नेताओं को JP और कर्पूरी की विचारधारा पढ़ाना।
फिर आज यह वैचारिक परंपरा कहाँ खो गई है?
आज बिहार की राजनीति पुनः जातीय जोड़तोड़, पद-प्राप्ति, और वोटबैंक के गणित में उलझी हुई है। विचार की जगह रणनीति ने ले ली है, और क्रांति की जगह सत्ता की चतुर चालें आ गई हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि बिहार फिर से खुद से पूछे-'मैं कौन हूँ?' क्या मैं महज जाति से पहचाना जाने वाला वोटर हूँ, या सामाजिक परिवर्तन का वाहक?
परंतु प्रश्न आज भी मौन नहीं हुआ है: 'मैं कौन हूँ?'
यह सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं, राजनीतिक भी है। यह सवाल आत्मचेतना से जुड़ा है, लेकिन साथ ही सामाजिक विघटन और पहचान की राजनीति की प्रतिक्रिया भी। दुर्भाग्यवश, आज उसी बिहार में जातिवादी ध्रुवीकरण ने इन पुरोधाओं की विचारधारा को हाशिये पर धकेल दिया है। सामाजिक न्याय के नाम पर जिस आंदोलन ने कभी ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी थी, आज वही आंदोलन जातीय पहचान की संकीर्ण राजनीति में सिमट कर रह गया है।
क्या यही थी कर्पूरी ठाकुर की ‘समता’ की कल्पना?
क्या नागार्जुन की कविताओं का ‘जनपक्ष’ यही था?
क्या जयप्रकाश का 'समाजवाद' इस तरह बंटवारे की रेखाओं पर टिका था?
इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, उनके सपनों में झांकना होगा। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान को सिरजते समय समानता की कल्पना की थी, जो हर नागरिक को जात-पात से ऊपर उठने का अधिकार देती है। लोहिया ने 'पिछड़ों को पचास' का नारा देकर समाज की ताकत को संतुलित करना चाहा, लेकिन इसका उद्देश्य सत्ता की लूट नहीं था, बल्कि समावेश था।
जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति केवल चुनावी परिवर्तन नहीं था, वह नैतिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों की पुर्नस्थापना की माँग थी। उन्होंने ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की बात की थी, न कि केवल सत्ता हस्तांतरण की। रेणु और नागार्जुन की कलम उस पीड़ा की गवाही देती थी, जो बिहार के गांवों में बसी थी-जहाँ किसान, दलित, स्त्रियां, वंचित और विस्थापित अपनी अस्मिता की खोज में संघर्षरत थे।
आज बिहार को फिर एक संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता
एक नई क्रांति जो ना केवल सामाजिक न्याय की बात करे, बल्कि न्याय के भीतर समावेश, समता और संवेदनशीलता भी लाए। जो ना केवल वंचितों को अधिकार दिलाए, बल्कि उन्हें नैतिक शक्ति से भी संपन्न करे। ऐसी क्रांति, जो यह समझे कि जाति केवल एक पहचान नहीं, एक दंश भी है, जिससे मुक्ति जरूरी है।
बिहार से ही उठना होगा वह स्वर
जो कहे -अब जातियों की गोलबंदी नहीं, विचारों की गोलबंदी होगी।
जो पूछे - किसने रोका कि दलित भी दीनदयाल बनें, मुसहर भी गांधी बनें, और मुसलमान भी जेपी बनें?
‘मैं कौन हूँ?’ इस प्रश्न की पुनः प्रासंगिकता
जब जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल में कहा था,'मैं कौन हूँ?' तो वह सत्ता के दमन के विरुद्ध नागरिक चेतना की पुकार थी। आज फिर यह प्रश्न उठाना ज़रूरी है, लेकिन इस बार जाति के जंजीरों से बाहर आकर।
क्या मैं सिर्फ अपनी जाति हूँ?
क्या मैं अपनी भाषा, अपने गाँव, अपने संविधान से नहीं जुड़ा?
क्या मेरे भीतर बुद्ध, भिखारी ठाकुर, दिनकर और रेणु की चेतना जीवित नहीं?
क्या मैं ब्राह्मण, यादव, दलित, कुशवाहा हूँ? -
या क्या मैं बुद्ध, भिखारी ठाकुर, दिनकर, और लोहिया का विचारधारात्मक वंशज हूँ?
यह प्रश्न हमें पुनः आत्म-पहचान की ओर ले जाएगा, जातिगत पहचान से नागरिक और मानवीय पहचान की ओर। अगर यह आत्म-चिंतन शुरू हुआ, तो न केवल बिहार बदलेगा, बल्कि भारत भी बदल सकता है। यह केवल जातियों को जोड़ने की नहीं, उन्हें पीछे छोड़ने की क्रांति होगी। बदल जाएगा एक उत्तर में, 'मैं वह हूँ जो न्याय चाहता है, बदलाव चाहता है, और बिहार को उस ऊँचाई पर देखना चाहता है जहाँ से कभी विचारों की नदियां बहा करती थीं।' बिहार, यह तुम्हारी परीक्षा है -इतिहास की नहीं, भविष्य की।
What's Your Reaction?