संवैधानिक विमर्श की नई दिशा : अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से राय के मायने
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े प्रश्नों पर राय मांगी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया जिसमें राज्यपालों को विधेयकों पर समय-सीमा में निर्णय लेने की बात कही गई थी। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी सार्वजनिक महत्व के संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट हर संदर्भ पर राय देने के लिए बाध्य नहीं है-खासकर जब मामला अस्पष्ट, राजनीतिक, या पहले से तय हो चुका हो। ऐतिहासिक रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश संदर्भों पर राय दी है, लेकिन सलाहकारी राय बाध्यकारी नहीं होती।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालयसे राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों (अनुच्छेद 200 और 201) से जुड़े कई सवालों पर राय माँगी है। यह संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के उस हालिया फैसले के बाद आया है जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय-सीमा तय की गई थी और ‘मानी गई सहमति’ (deemed consent) की अवधारणा पेश की गई थी, ताकि विधायी बिलों पर राज्यपालों की निष्क्रियता का समाधान हो सके।

अनुच्छेद 143 क्या है?
अनुच्छेद 143(1) के तहत, राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न पर राय माँग सकते हैं, जो जनहित में हो या सार्वजनिक महत्व का हो। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई करनी होती है और अपनी राय राष्ट्रपति को देनी होती है। यह सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार (advisory) अधिकारिता का हिस्सा है, जो केवल राष्ट्रपति के लिए है।
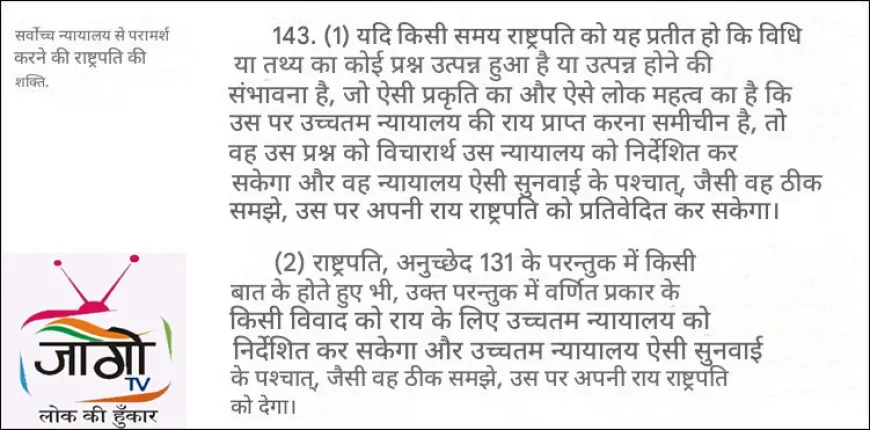
ऐतिहासिक संदर्भ
संविधान लागू होने के बाद से अब तक एक दर्जन से अधिक बार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143(1) का उपयोग किया गया है। प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं:
- 1951: दिल्ली लॉज एक्ट, अजमेर-मेरवाड़ा एक्ट और पार्ट C स्टेट्स (लॉज) एक्ट से जुड़े विधायी शक्तियों के हस्तांतरण पर पहला संदर्भ।
- 1958: केरल एजुकेशन बिल, 1957 के कुछ प्रावधानों की वैधता पर।
- 1961: भारत-पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत भूमि हस्तांतरण (बेरुबारी यूनियन)।
- 1963: अनुच्छेद 289 के तहत राज्यों की संघीय कराधान से छूट।
- 1974: राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर।
- 1978: स्पेशल कोर्ट्स बिल की वैधता।
- 1993: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद।
- 2012: 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामला।
- 2025: राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर सहमति देने की समय-सीमा।
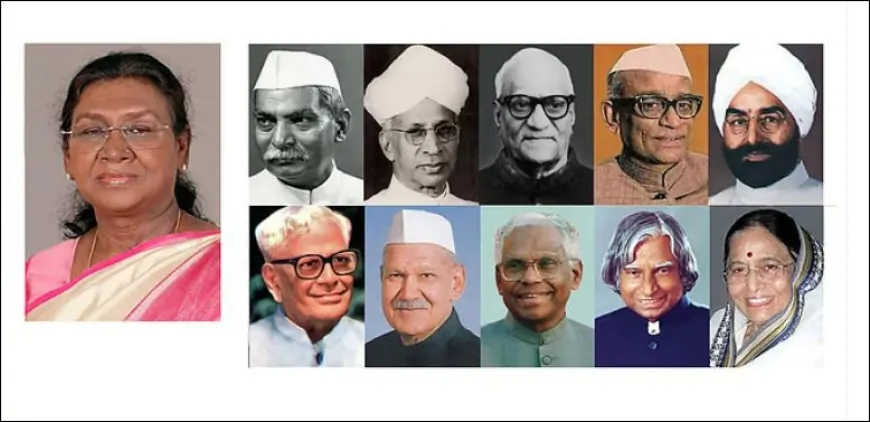
सर्वोच्च न्यायालयकी राय और सीमाएँ
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143(1) के तहत दी गई राय बाध्यकारी (binding) नहीं होती, बल्कि सलाहात्मक (advisory) होती है।
- कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह हर संदर्भ पर राय देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कोई प्रश्न अस्पष्ट, व्यापक या संविधान से असंबंधित है, तो कोर्ट उसे अनुत्तरित छोड़ सकती है।
- यदि कोई मामला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय में तय हो चुका है, तो उसी विषय पर अनुच्छेद 143 के तहत दोबारा राय नहीं माँगी जा सकती।
- कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि संदर्भ केवल राजनीतिक या सामाजिक-आर्थिक विषयों से जुड़ा है और उसमें कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, तो ऐसे मामलों में राय देने से इनकार किया जा सकता है।
वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रपति का कदम
राष्ट्रपति मुर्मू ने 14 सवालों के साथ सर्वोच्च न्यायालय से पूछा है कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है, जबकि संविधान में ऐसी कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं है। यह पहली बार है जब राष्ट्रपति मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) का उपयोग किया है, और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भी यह पहली घटना है।

What's Your Reaction?














































































































































































