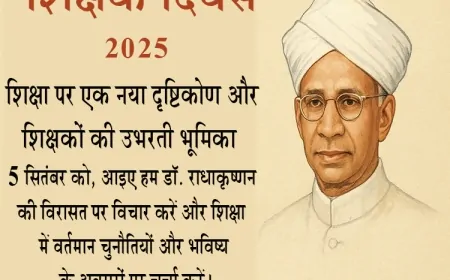43 साल की सजा, 104 साल की उम्र: लखन की रिहाई और वैश्विक न्यायिक व्यवस्था पर एक चिंतन
104 वर्षीय लखन सरोज को 43 साल जेल में बिताने के बाद 2 मई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। 1977 में हत्या के आरोप में सजा पाने वाले लखन की रिहाई ने भारत की न्यायिक देरी और गलत सजा की समस्या को उजागर किया। उनकी बेटी आशा ने इसे सुकून की बात बताया। यह मामला वैश्विक न्यायिक सुधारों, जैसे अमेरिका और यूके के उदाहरणों, से सीख लेकर भारत में समयबद्ध और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल देता है।

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के गैराए गाँव के 104 वर्षीय लखन सरोज की कहानी न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि वैश्विक न्यायिक व्यवस्थाओं की कमियों और सुधार की आवश्यकता को उजागर करने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। 1977 में हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार लखन को 1982 में प्रयागराज के जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 43 साल जेल में बिताने के बाद, 2 मई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। उनकी बेटी आशा ने कहा, "43 साल का दाग आखिरकार मिट गया। अब वह सुकून से इस दुनिया से जा सकते हैं।" यह घटना भारत की न्यायिक प्रणाली में देरी और वैश्विक स्तर पर न्यायिक सुधारों की जरूरत को रेखांकित करती है।
लखन का मामला: एक व्यक्तिगत त्रासदी
लखन, जो 4 जनवरी 1921 को पैदा हुए, को 1977 में एक सामूहिक झगड़े में प्रभु सरोज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चार अभियुक्तों में से तीन की अपील की प्रक्रिया के दौरान मृत्यु हो गई, और लखन अकेले इस लंबी कानूनी लड़ाई को झेलते रहे। उनकी रिहाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सहयोग से संभव हुई, लेकिन यह देरी से आई। उच्च न्यायालय के आदेश को जेल तक पहुंचने में 18 दिन और लग गए। लखन की शारीरिक स्थिति अब कमजोर है; उनकी बेटी के अनुसार, वह लगातार पैर दर्द से पीड़ित हैं और दैनिक कार्यों के लिए सहायता की जरूरत है। यह मामला न केवल न्यायिक देरी, बल्कि जेल में बिताए गए दशकों के शारीरिक और मानसिक प्रभाव को भी दर्शाता है।
भारत की न्यायिक व्यवस्था: समस्याएँ और चुनौतियाँ
भारत में न्यायिक देरी एक पुरानी समस्या है। मार्च 2022 तक, देश भर के न्यायालयों में 4.7 करोड़ मामले लंबित थे, जिनमें से 59 लाख उच्च न्यायालयों में और 70,000 से अधिक सर्वोच्च न्यायालय में थे। लखन का मामला इस बात का प्रतीक है कि "न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है।" भारत की न्यायिक प्रणाली की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं:
- न्यायाधीशों की कमी: 25 उच्च न्यायालयों में स्वीकृत 1,104 न्यायाधीशों के पदों में से 387 रिक्त हैं। यह कमी मामलों के निपटारे की गति को धीमा करती है।
- अधिकारियों की लापरवाही: लखन के मामले में, रिहाई के आदेश को लागू करने में 18 दिन की देरी प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाती है।
- अंडर-ट्रायल कैदियों की भीड़: 1970 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 52% जेल कैदी अंडर-ट्रायल थे। यह संख्या आज भी चिंताजनक है।
- जेल सुधारों की कमी: जेलों में भीड़भाड़, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ , और कैदियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों की कमी स्थिति को और गंभीर बनाती है।
लखन जैसे मामले यह सवाल उठाते हैं कि क्या हमारी न्यायिक प्रणाली वास्तव में निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय प्रदान करने में सक्षम है।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य: अन्य देशों के उदाहरण
वैश्विक स्तर पर भी न्यायिक देरी और गलत सजा के मामले देखे गए हैं, जो भारत के लिए सबक हो सकते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका: 1989 में सेंट्रल पार्क फाइव मामले में पांच किशोरों को गलत तरीके से बलात्कार और हमले के लिए दोषी ठहराया गया। 2002 में, डीएनए साक्ष्य और असली अपराधी के कबूलनामे के बाद उन्हें बरी किया गया। इस मामले ने नस्लीय पक्षपात और जल्दबाजी में सजा देने की समस्या को उजागर किया। अमेरिका ने इसके बाद डीएनए टेस्टिंग और मुआवजा नीतियों को मजबूत किया।
- यूनाइटेड किंगडम: गिल्डफोर्ड फोर (1974) में चार लोगों को गलत तरीके से आतंकवादी बम विस्फोट के लिए दोषी ठहराया गया। 1989 में उनकी रिहाई के बाद, यूके ने आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र आयोग (CCRC) की स्थापना की। यह भारत के लिए एक मॉडल हो सकता है।
- जापान: जापान में हाकमदा इवाओ को 1968 में हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और 2014 में डीएनए साक्ष्य के आधार पर रिहा किया गया। इस मामले ने जापान की कठोर पूछताछ प्रणाली और गलत सजा की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया।
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि न्यायिक सुधार, स्वतंत्र समीक्षा तंत्र, और वैज्ञानिक साक्ष्य का उपयोग गलत सजा को कम कर सकता है।
भारत के लिए सबक और सुझाव
लखन का मामला भारत की न्यायिक और जेल प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। निम्नलिखित सुझाव लागू किए जा सकते हैं:
- न्यायाधीशों की भर्ती और प्रशिक्षण: रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए और न्यायाधीशों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए।
- तकनीकी उपयोग: ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई को पूरे देश में सामान्य किया जाए, लेकिन साथ ही मामलों के तेजी से निपटारे के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए।
- स्वतंत्र समीक्षा आयोग: गलत सजा की समीक्षा के लिए यूके की तरह एक स्वतंत्र आयोग स्थापित किया जाए।
- मुआवजा नीति: रुदुल साह मामले (1983) में शुरू हुई मुआवजा परंपरा को मजबूत किया जाए। लखन जैसे कैदियों को उनकी खोई जिंदगी के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास सहायता दी जाए।
- जेल सुधार: जेलों में भीड़भाड़ कम करने, चिकित्सा सुविधाएँ बढ़ाने, और कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएँ।
- सार्वजनिक जागरूकता: सोशल मीडिया और मीडिया ने लखन के मामले को उजागर किया। ऐसी पहल को प्रोत्साहित किया जाए ताकि अन्याय के मामले सामने आएँ ।
लखन की रिहाई एक कड़वी जीत है। 43 साल की कैद ने उनकी जवानी, परिवार, और सम्मान छीन लिया। उनकी बेटी आशा के शब्दों में, "वह अब सुकून से जा सकते हैं," लेकिन यह सुकून अधूरा है। भारत की न्यायिक व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और लखन 43 साल तक सलाखों के पीछे न रहे। वैश्विक उदाहरणों से सीख लेते हुए, भारत को अपनी न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी, समयबद्ध, और निष्पक्ष बनाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। लखन की कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल बरी करना नहीं, बल्कि समय पर और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना है।
What's Your Reaction?